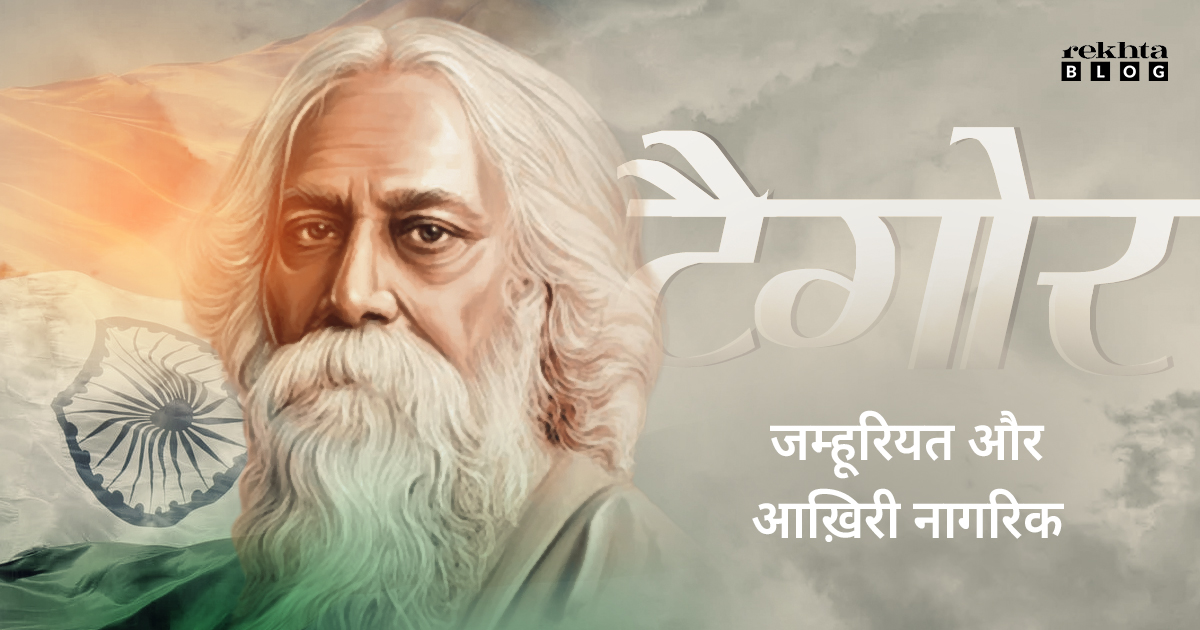
टैगोर, जम्हूरियत और आख़िरी नागरिक
पिछले बरस एक ख़बर दिखी, अफ़्ग़ानिस्तान में रह रहे आख़िरी यहूदी की। मज़हबी शिद्दत-पसंदी, इंतिशार, जंग, इन सब अस्बाब की वजह से रफ़्ता रफ़्ता अफ़्ग़ानिस्तान में रहने वाले यहूदी मुल्क छोड़ के चले गए सिवाए एक के। आज उस मुल्क में सिर्फ़ एक यहूदी है जो परेशानियाँ उठा कर अपनी इबादत करता है, अपनी इबादत-गाह का ख़याल रखता है, यहूदी तर्ज़-ए-ज़िंदगी गुज़ारता है और इस वजह से मुसीबतें भी उठाता है। अफग़ानिस्तान में पिछले साल कहने के लिए जम्हूरियत भी थी लेकिन वहाँ से बिछड़े हुए यहूदी वापस नहीं आना चाहते थे।
ये ख़बर पढ़ते ही गुरू देव रबीन्द्रनाथ टैगोर का नज़्म ज़ेहन में घूम गया।
“where the mind is without fear”
जम्हूरियत को अगर सिर्फ़ वोट करने के हक़ से ता’बीर किया जाए तो उसका मतलब ये होगा कि मुल्क में अक्सरिय्यती ख़याल, वो सोच जिस के मानने वाले अक्सरिय्यत में हों उस सोच को ही ग़लबा मिलेगा। लेकिन इस का दूसरा पहलू क्या ये है कि बाक़ी तमाम ख़याल, बाक़ी तमाम लोग और तमाम फ़िक्र के लोगों के लिए कोई जगह नहीं?
टैगोर की नज़्म की पहली लाइन में ही साफ़ है कि टैगोर जो आदर्श समाज चाहते हैं उसकी पहली शर्त दिल-ओ-दिमाग़ में ख़ौफ़ न होना है।
Where the mind is without fear…..
हर कोई बिना किसी ख़ौफ़ या डर के बिना किसी दूसरे को परेशान किए अपनी ज़िन्दगी जैसे चाहे वैसे जीने के लिए आज़ाद हो। आज़ादी-ए-ख़याल, बोलने की आज़ादी, और तमाम वो आज़ादियाँ जो एक सोचने समझने वाले मुआ’शरे की ज़रूरत हैं वो उसे हासिल हों बिना किसी ख़ौफ़ के। ज़ेहन बे-ख़ौफ़ हो कर ख़ुद का इज़हार कर सके।
“And the head is held high”
जहाँ सम्मान के साथ जीने के लिए सिर्फ़ इंसान होना काफ़ी हो, पैसा, दौलत, रुत्बा, मज़हब, ज़ात, वग़ैरा जैसी चीज़ों के होने न होने से नागरिक होने के सम्मान पर कोई फ़र्क़ न पड़े। एक फ़क़ीर को भी इंसान होने के नाते वो ही सम्मान मिले जो एक सेठ को मिलता है।
“Where knowledge is free”
टैगोर के मिसाली समाज में देश में विद्या मूलभूत सुविधा होगी, जो सब को समान रूप से मिलेगी, ख़रीदी जा सकने वाली चीज़ नहीं होगी ये। विद्या आदर्श मुल्क का कारण भी होगी और आदर्श देश का अभिन्न अंग भी। यही सबब भी होगी यही मुसब्बब भी।

“Where the world has not been broken up into fragments
By narrow domestic walls”
जहाँ ज़मीनों को बाँटा ना गया हो दीवारों से सरहदों से। ज़ाहिर है टैगोर शायर थे, टैगोर की ज़मीन दिल है और दिलों के बीच की दीवार वो नफ़रतें हैं या मोहब्बतें हैं जो हमें दूसरों से अलग करती हैं, ये मेरे मोहल्ले वाले ये दूसरे मोहल्ले के, ये मेरे मज़हब वाले ये मुख़्तलिफ़ मज़हब वाले, ये मेरे मुल्क वाले ये पराए मुल्क के, ये मेरी ज़बान वाले ये विदेशी ज़बान वाले, ये सारी सरहदें अपनी चीज़ से मोहब्बत के साथ दूसरे को कब पराया कर देती हैं पता ही नहीं चलता। एक मिसाली मुआ’शरा एक ऐसे हसीन बाग़ीचे की तरह होता है जहाँ सैकड़ों रंग हों लेकिन वो सब आपस में ऐसे मिल गए हों कि हर रंग दूसरे का पूरक हो, उन सब के मिलने से आँख को हुस्न मिले और दिल को सुकून। सरहदों की वज्ह से मोहब्बत और आलमी भाई-चारे में बटवारा नहीं होगा।
“Where words come out from the depth of truth”
जहाँ लफ़्ज़ हक़ और सत्य के परवरदा हों, उनकी बुनियाद सच्चाई हो, उनकी वजह सत्य हो, उनका मक़सद भी हक़ हो। मक्कारी, तशद्दुद, नफ़रत, चोट पहुँचाना उनका न मक़सद हो न ही उनकी बुनियाद हो।
ग़ालिबन हज़रत अली का क़ौल है:-
जराहत-उस-सिनान लहल-तियाम
वला-यलतइम मा-जरह-अल-लिसान
यानी ख़ंजर का लगाया हुआ ज़ख़्म भर जाता है मगर वो ज़ख़्म नहीं भरता जो ज़बान ने लगाया हो।

टैगोर के मआशरे में लफ़्ज़ एक ऐसी इकाई है जो ब-ज़ाहिर बहुत छोटी है मगर एक पूरी दुनिया बना सकती है मोहब्बत की बुनियाद पर।
“Where tireless stretching reaches its arms towards perfection”
जहाँ अन-थक मेहनत सिर्फ़ इस बात के लिए हो कि उस मिसाली मुआ’शरे की इंतिहा को पाया जा सके। कमाल की हद को पहुँचा जा सके। ये कमाल रुपये पैसे से हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि इंसाफ़, मोहब्बत, एकता और अपनाइयत के रास्ते से हासिल होगा।
“Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert of dead habit”
जहाँ बरसों से चले आ रहे पूर्वाग्रहों और मुग़ालतों की वजह से अक़्ल ने रास्ता ना भटका हो, और मंतिक़ और तार्किकता का रास्ता जारी रहे। क्योंकि अक़्ल ही है जो अस्ल फ़ैसल है जो अस्ल रहबर है।
“Where the mind is led forward by thee
Into ever-widening thought and action
Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.”
ऐ ख़ुदा जहाँ ज़ेह्न की रहनुमाई तू करे
ऐसे मुआ’शरे में मेरा मुल्क बे-दार रहे
पहले अज़ादी की बात की, इल्म की बात की, साइंटिफ़िक टेम्पर की बात की, मंतिक और तर्क की बात की, उसके फ़ौरन बाद ख़ुदा को, ईश्वर को रहनुमा बनाने की बात कही, यानी वो ख़्याल जो किसी से नफ़रत करना सिखाए, वो इल्म जो किसी ज़ुल्म का रास्ता हमवार करे, वो तार्किकता और वो अक़्ल जिममें संवेदना न हो, वो दलीलें जो ग़रीब से रोटी छीनने को भी न्यायसंगत बता सकें ऐसी दलीलें और ऐसी तार्कीकता उस समाज की बुनियाद नहीं होगी, बल्कि उस इल्म, उस फ़िक्र, तार्किकता और उस मंतिकी तर्ज़-ए-अमल का मक़सद ही होगा कि ईश्वर के सब बन्दे हैं तो आख़िरी बंदे और आख़िरी नागरिक को भी इज़्ज़त के साथ रहने का हक़ मिले, ज़िन्दगी की ख़ूबसूरती देखने का मौक़ा मिले, आख़िरी नागरिक भी आख़िरी न समझे ख़ुद को।

यही हमारी संविधान की आत्मा है, यही संविधान की प्रस्तावना का मूल है और यही वो समाज है जिसका ख़्वाब हमारे बड़ों ने देखा था।
टैगोर की इस कविता का मैंने मंज़ूम उर्दू तर्जुमा (काव्य अनुवाद) किया था, मालूम नहीं कि इस कविता की आत्मा को अनुवाद में कितना ला पाया हूँ। बहर हाल ये है वो अनुवाद:
जहाँ फ़िक्र-ए-इन्साँ को हैबत न हो
जहाँ सर उठाने पे तोहमत न हो
सभी चशमा-ए-इल्म से पी सकें
जहाँ इल्म पाबन्द-ए-दौलत न हो
फ़सीलों नें बाँटी न हो ये ज़मीं
खिले हक़ की टहनी पे लफ़्ज़-ए-हसीं
हो काविश की बाहों में हुस्न-ए-कमाल
भटक कर न हो अक़्ल सहरा-नशीं
जहाँ रहबर-ए-ज़हन तू ही रहे
बढ़े हद्द-ए-फिक्र-ओ-अमल फिर बढ़े
इसी ख़ुल्द की सुब्ह में ऐ ख़ुदा!!
मिरा मुल्क जागे, मिरी शब ढले
NEWSLETTER
Enter your email address to follow this blog and receive notification of new posts.




