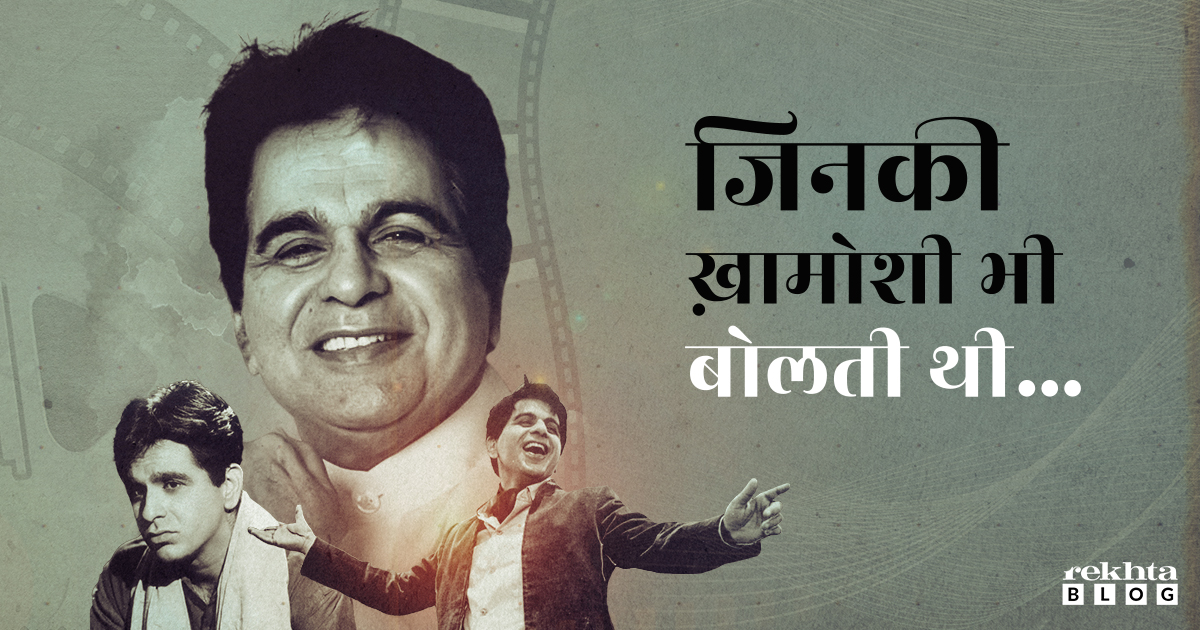
दिलीप कुमार: एक ज़िन्दगी के भीतर कितनी ज़िन्दगियां…
मैं बहुत बार हैरान होता हूँ कि उस इनसान ने एक ही ज़िन्दगी में कितनी ज़िंदगियां जी ली होंगी। भले ही वह कैमरे के सामने हो, कितनी बार अभिनय में ही सही वह मौत के करीब तक जाकर लौट आया होगा। ‘देवदास’ में भागती ट्रेन में मौत की देहरी पर वह आर्त पुकार। हर बार मर के जी उठना और फिर एक नई मृत्यु की तरफ कदम बढ़ा लेना। प्रेम और बिछोह के कितने दरवाजों से होकर गुज़रना, किसी और के ग़ुस्से और नफ़रत की देहरियों को बार-बार लांघना। प्रतिशोध की खामोश आँच को कितनी ही बार चुपचाप सहना और बस अपनी आँखों से बयां करना। एक चेहरे में कितने रिश्तों की परछाइयों जज़्ब कर लेना। उनकी शख़्सियत में आखिर ऐसा कौन सा जादू था कि जब वे सिनेमा के फ़्रेम में होते तो कोई चुंबकीय आकर्षण हमें बांध लेता था?
दिलीप कुमार इकलौते अभिनेता थे कि जब कैमरे की तरफ़ पीठ होती थी तब भी वे अभिनय करते नजर आते थे। फ़िल्म ‘अमर’ में एक दृश्य में मधुबाला उनसे मुख़ातिब हैं और कहती हैं, “सूरत से तो आप भले आदमी मालूम होते हैं…” फ़्रेम में सिर्फ़ उनकी धुंधली सी बांह नज़र आती है मगर संवाद अदायगी के साथ वे जिस तरीक़े से अपनी बांह को झटके से पीछे करते हैं वह उनके संवाद “सीरत में भी कुछ ऐसा बुरा नहीं…” को और ज़ियादा असरदार बना देता है। उस दौर के और बाद के दौर में भी ज़ियादा अभिनेता अपने किसी ख़ास मैनरिज़्म से पहचाने जाते थे। दिलीप कुमार के पास ऐसा कोई मैनरिज़्म नहीं था जिसकी आसानी से नक़ल की जा सके। चालीस के दशक से लेकर सत्तर तक जब लाउड एक्टिंग का दौर था, वे उन गिने-चुने अभिनेताओं में थे जिनकी ख़ामोशी बोलती थी। आप बिना ऊबे हुए देर तक स्क्रीन पर उन्हें ख़ामोश देख सकते हैं।
बहुत सी फ़िल्मों में इस ख़ामोशी का उन्होंने बहुत असरदार इस्तेमाल किया है। ‘शक्ति’ फ़िल्म के कई दृश्यों में उनकी इस बोलती हुई ख़ामोशी को देखा जा सकता है। याद करें राखी की मृत्यु के बाद का वह दृश्य जब अमिताभ को पुलिस लेकर आती है और वे अपने दोनों हाथों से पिता की बांह थाम लेते हैं। इस दृश्य में कोई किसी से कुछ नहीं बोलता, मगर दिलीप कुमार जिस नज़र से अमिताभ की तरफ़ देखते हैं और फिर अपनी हथेली से आँखों को ढक लेते हैं, उस पर कई पन्ने लिखे जा सकते हैं।
आख़िर दिलीप का स्क्रीन पर आना इतना बांधने वाला क्यों होता था? इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनकी सिनेमा की समझ बहुत गहरी थी। अगर आप ग़ौर करें तो हर फ़्रेम, हर शॉट का वे बड़ी समझदारी से अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लेते थे। दूसरी ख़ूबी यह थी कि वे पूरे शरीर से अभिनय करते थे। चालीस के दशक के ज़ियादातर दूसरे अभिनेता जहां कैमरे के सामने सिर्फ़ खड़े होकर अपने संवाद बोलते थे, दिलीप कुमार बहुत छोटी-छोटी शारीरिक हरकतों से अपने फ़्रेम को गतिशील बना देते थे।

जहां पारसी थिएटर के असर में अभिनेता बहुत लाउड ढंग से अभिनय करते थे, दिलीप कुमार हर फ़िल्म में अपने किरदार के हिसाब से वे अपनी भंगिमाओं का चयन करते थे और बहुत ही बारीकी से अपने किरदार को सजाते थे। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण जिया सरहदी की फ़िल्म ‘फ़ुटपाथ’ में दिखता है। फ़िल्म के पहले ही दृश्य में वे जिस तरह अपनी कुर्सी से उठते है, अगली अलमारी तक जाते हैं, फ़ाइल रखते हैं, वापस लौटते हैं और बात करते-करते दूसरी अलमारी पर हाथ टिकाकर खड़े होते हैं, अपने हाथों से अपनी आँखें बंद करते हैं और अचानक अपनी भंगिमा बदलते हैं, एक साथ कई बातें कह जाता है। अख़बार के दफ्तर का एक मुलाज़िम, उसके भीतर का आक्रोश, दुनिया को देखने का उसका नज़रिया, अपनी नौकरी और काम के बारे में उसकी सोच, खुद के आर्थिक हालात – सब कुछ दो मिनट के इस दृश्य में वे स्पष्ट कर देते हैं।
जावेद अख़्तर ने एक इंटरव्यू में कहा था, “पूरी दुनिया में फ़िल्मों में अगर कोई पहला मेथड एक्टिंग करने वाला अभिनेता था तो वे दिलीप साहब ही थे। हालांकि, आम तौर पर मार्लन ब्रांडो को पहला मेथड एक्टर समझा जाता है, लेकिन वे करिअर में दिलीप साहब से सात-आठ साल जूनियर थे। “मेथड एक्टिंग को 20वीं सदी के महान अभिनेता ली स्ट्रासबर्ग प्रचलन में लाए थे इसलिए इसे स्ट्रासबर्ग की तकनीक भी कहा जाता है। मेथड एक्टिंग स्तानिस्लाव्स्की और मास्को आर्ट थिएटर से प्रभावित थी। जिसमें अभिनेता अपने किरदार में कुछ इस प्रकार घुल-मिल जाता था कि स्क्रीन पर वो किरदार ही नजर आए।
दिलीप कुमार को इस संदर्भ में समझना हो तो उनकी दो फ़िल्में एक के बाद एक देखनी चाहिए, पहली मुगल-ए-आज़म और दूसरी गंगा-जमना। एक में वे शहज़ादे बने हैं तो दूसरे में गांव का एक गंवार। रेहान फज़ल बीबीसी में लिखते हैं, “मुग़ल-ए-आज़म फ़िल्म में पृथ्वीराज कपूर का चरित्र ख़ासा प्रभावी और लाउड था। शहज़ादा सलीम की भूमिका में कोई और अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के सामने उतना ही लाउड होने का लोभ संवरण नहीं कर पाता लेकिन दिलीप कुमार ने जानबूझ कर बिना अपनी आवाज़ ऊँची किए हुए अपनी मुलायम, सुसंस्कृत लेकिन दृढ़ आवाज़ में अपने डायलॉग बोले और दर्शकों की वाहवाही लूटी।”

अपने कॉलेज के दिनों में क्रिकेट और फुटबॉल से उनका लगाव लगता है बाद में भी उनके काम आया। उनके चलने के अंदाज़ में एक क़िस्म का फुर्तीलापन था। जरा ‘मधुमती’ के गीत “आजा रे परदेसी में” पहाड़ी ढलान पर पेड़ों के बीच उतरते हुए दिलीप कुमार को याद कीजिए। स्टूडियो सिस्टम वाली पुरानी फ़िल्मों में जब अभिनेताओं के पास मूवमेंट की बहुत ज़ियादा गुंजाइश नहीं होती थी, दिलीप कुमार एक खास तरह की ऊर्जा से भरे हुए नज़र आते थे। हाथों के मूवमेंट, देखने का तरीका, कब मुड़ना है, लंबे संवादों में कितनी देर कहां देखना है, फ़्रेम के किस हिस्से में रहते हुए क्या करना है… इसका उनको बखूबी अंदाज़ था। बांबे टॉकीज के शुरुआती दिनों में वे फ़िल्म की कहानी तथा दूसरे तकनीकी पहलुओं में काफ़ी दिलचस्पी लेते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि अपने समय के वे इकलौते ऐसे अभिनेता थे, जो कैमरा मूवमेंट और फ़्रेम के एक-एक सेकेंड का इस्तेमाल कर लेते थे।
शुरुआती कुछ फ़्लॉप फ़िल्मों के बाद दिलीप ने यह समझ लिया कि उन्हें अभिनय के लिए ख़ुद ही रास्ता बनाना होगा। जब 1951 में फ़िल्म ‘दीदार’ आयी थी तो उसमें उन्होंने एक अंधे व्यक्ति का किरदार निभाया था। उन्होंने इस किरदार को स्क्रीन पर लाने से पहले कई दिनों तक बांबे के महालक्ष्मी स्टेशन के पास एक अंधे फ़कीर के हाव-भाव को ग़ौर से देखना शुरू किया, उससे दोस्ती की और एक बहुत बारीक सी बात पकड़ी कि अंधे व्यक्ति का अभिनय करते समय अभिनेता की आँखों में कोई भाव नहीं आना चाहिए।
“मधुबन में राधिका नाचे रे” गीत के फ़िल्मांकन के लिए उनका सितार सीखना और ‘नया दौर’ के लिए तांगा चलना तो एक किंवदंती बन चुका है, कहते हैं कि दिलीप कुमार ने यह बात भी पकड़ी कि जब कोई सितार बजाता है तो उसके तार चुभते हैं और उससे चेहरे पर हल्की सी शिकन आती है तो इस गाने में उस शिकन को देखा जा सकता है। वहीं अपनी आत्मकथा में दिलीप कुमार बताते हैं कि जब ‘मशाल’ फ़िल्म में जब वे सूनी सड़क पर अपनी बीमार पत्नी को अस्पताल पहुँचाने के लिए गुहार लगा रहे होते हैं तो दरअसल उनकी स्मृतियों में अपने पिता कौंध गए होते हैं, जब उनकी मां बीमार थीं और वे इसी तरह घबराए हुए थे।
किरदारों मे डूब जाने की कला के पीछे एक और बात थी और वह थी दुनिया के श्रेष्ठ क्लासिक साहित्य से उनकी वाक़फ़ियत। कॉलेज के दिनों में उन्होंने मोपांसा की कहानियों को पढ़ना शुरू किया और फिर पढ़ने-पढ़ाने का यह सिलसिला जीवन भर चलता रहा। सायरा बानो उनकी आत्मकथा की भूमिका में उनकी लाइब्रेरी का खास तौर पर जिक्र करती हैं और किताबों के शौक़ के बारे में भी बताती हैं। क्लासिक लिटरेचर और बायोग्राफ़ी में उनकी ख़ासी दिलचस्पी थी। मोपांसा के बाद उनकी पसंद के लेखकों में दोस्तोएवस्की और यूजीन ओ’ नील जैसे लेखक भी शामिल हो गए। यह अनायास ही नहीं है कि हिंदुस्तान का ट्रेजडी किंग कहा जाने वाला लेखक दोस्तोएवस्की को पढ़ता था और यह भी संभव नहीं था कि दोस्तोएवस्की को पढ़ने वाला कैमरे के सामने किसी किरदार को प्रस्तुत करने में कैसा भी हल्कापन दिखाए।

दिलीप कुमार सिर्फ़ ट्रेजडी किंग नहीं थे। अमिताभ बच्चन के आने से बहुत पहले वे अपने क़िस्म के एक एंग्री-मैन थे। उनके पास एक शानदार विद्रोही तेवर था। यह देवदास फ़िल्म की बुझी राख जैसा ग़ुस्सा नहीं था, बल्कि उसमें एक लाउडनेस एक मुखरता थी। चाहे ‘सगीना महतो’ हो, ‘गंगा जमना’, ‘दिल दिया दर्द लिया’ हो या फिर ‘राम और श्याम’। ये सभी एक अंडरडॉग के उठ खड़े होने की कहानियां थीं। प्रतिरोध उनकी आँखों में बोलता था। फ़िल्म ‘मजदूर’ और ‘मशाल’ में दिलीप कुमार ने भीतर के इसी प्रतिरोध को और ज्यादा विस्तार दिया है।
‘मशाल’ और ‘शक्ति’ फ़िल्म में उन्होंने अपने जीवन के उत्तरार्ध का सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया है। यहां दिलीप कुमार जैसे ख़ुद के किरदार को स्क्रीन पर उतारते हैं। एक पूराने मूल्यों पर यकीन करने वाला इनसान उस दुनिया से टकराता है जो बदल रही है। उनका ग़ुस्सा किस तरह से हताशा में बदलता है, इसे वे बख़ूबी अपने अभिनय में उतार पाए हैं। फ़िल्म चाहे कितनी भी मेलोड्रामाटिक हो, दिलीप कुमार को पता था कि ड्रामा किस तरह उनके दर्शकों अपनी गिरिफ़्त में लेगा और वे स्तब्ध से उनको देखते रह जाएंगे।
दिलीप ने यह साबित किया कि वे स्क्रीन पर किरदार को जीते थे। आज से कई बरस बाद भी जब हम उन फ़िल्मों को देखेंगे तो यह यकीन करना मुश्किल होगा कि कभी ऐसा कोई शख़्स इस दुनिया में था, जिसने हर किरदार को ऐसी शिद्दत के साथ जिया है कि इतनी शिद्दत से तो लोग बाग अपनी जिंदगी भी नहीं जीते हैं।
NEWSLETTER
Enter your email address to follow this blog and receive notification of new posts.




