
इब्न-ए-इंशा और उनका चाँद नगर
चाँद हमेशा से हमारी उर्दू शायरी का एक बेहद अहम किरदार रहा है और चाँद के मौज़ूअ पर हज़ार-हा शेर हमारे शायरों ने मुख़्तलिफ़ हवालों से कहे हैं। चाँद के कितने ही किरदार हैं। कभी चाँद माशूक़ की मिसाल बन जाता है, तो कभी माशूक़ से रश्क करने वाला बन जाता है। चाँद से मुतअल्लिक़ बहुत सारे मुहवारे भी हमारी ज़बान का हिस्सा हैं, मसलन ईद का चाँद होना, चार चाँद लगना वग़ैरह। इसके बावजूद जब मैं चाँद के हवाले से शायरी की बात करता हूँ तो मेरे ज़हन में सिर्फ़ दो नाम नुमायाँ होते हैं – पहला मीर तक़ी मीर और दूसरा इब्न-ए-इंशा। मीर की चाँद से निस्बत के क़िस्से मशहूर-ए-ज़माना हैं। मीर की एक इश्क़िया मसनवी ‘ख़्वाब-ओ-ख़याल’ से ये शेर देखें :
नज़र रात को चाँद पर गिर पड़ी
तो गोया कि बिजली सी दिल पर पड़ी
नज़र आई इक शक्ल महताब में
कमी आई जिस से ख़ुर-ओ-ख़्वाब में
अगर-चंद परतव से मह के डरूँ
व-लेकिन नज़र उस तरफ़ ही करूँ

मीर के शायरी में चाँद से निस्बत के हवाले से और कितने ही इक़्तिबास दिए जा सकते हैं। इसी को मौज़ूअ बनाते हुए अहमद फ़राज़ का शेर “आशिक़ी में मीर जैसे ख़्वाब मत देखा करो, बावले हो जाओगे महताब मत देखा करो” बेहद मक़बूल है। इब्न-ए-इंशा की शायरी के हवाले से बात करें, तो न उन्हें सिर्फ़ चाँद से निस्बत नज़र आती है, बल्कि उनके अशआर में उनकी मीर से अक़ीदत को साफ़ तौर पर देखा जा सकता है। इब्न-ए-इंशा का शेर है :
अल्लाह करे ‘मीर’ का जन्नत में मकाँ हो
मरहूम ने हर बात हमारी ही बयाँ की
‘मीर’ को अपना मौज़ूअ बना कर कहे गए अशआर की तादाद इब्न-ए-इंशा की शायरी में बहुत ज़ियादा है। कुछ शेर और देखें :
कभी ‘मीर’ फ़क़ीर की बैतों से, कभी ‘इंशा’-जी की ग़ज़लों से
इन बिरह की बेकल रातों में, हम जोत जगाते हैं मन में
अब क़ुरबत-ओ-सोहबत-ए-यार कहाँ, लब-ओ-आरिज़-ओ-ज़ुल्फ-ओ-कनार कहाँ
अब अपना भी ‘मीर’ सा आलम है, टुक देख लिया, जी शाद किया
मीर का ज़िक्र तो उनकी शायरी में आया ही है लेकिन सिर्फ़ जगह-जगह मीर की शायरी का भी रंग उनकी शायरी में नज़र आता है। उस्लूबी सत्ह पर इब्न-ए-इंशा और मीर की शायरी में कोई मुमासिलत नज़र नहीं आती लेकिन मानवी एतिबार से इब्न-ए-इंशा की शायरी में मीर की छाप दिखाई देती है। इब्न-ए-इंशा का एक शेर है :
कभी बस्तियाँ-बन, कभी कोह-ओ-दमन, रहा कितने दिनों यही जी का चलन
जहाँ हुस्न मिला वहाँ बैठ रहे, जहाँ प्यार मिला वहाँ साद किया
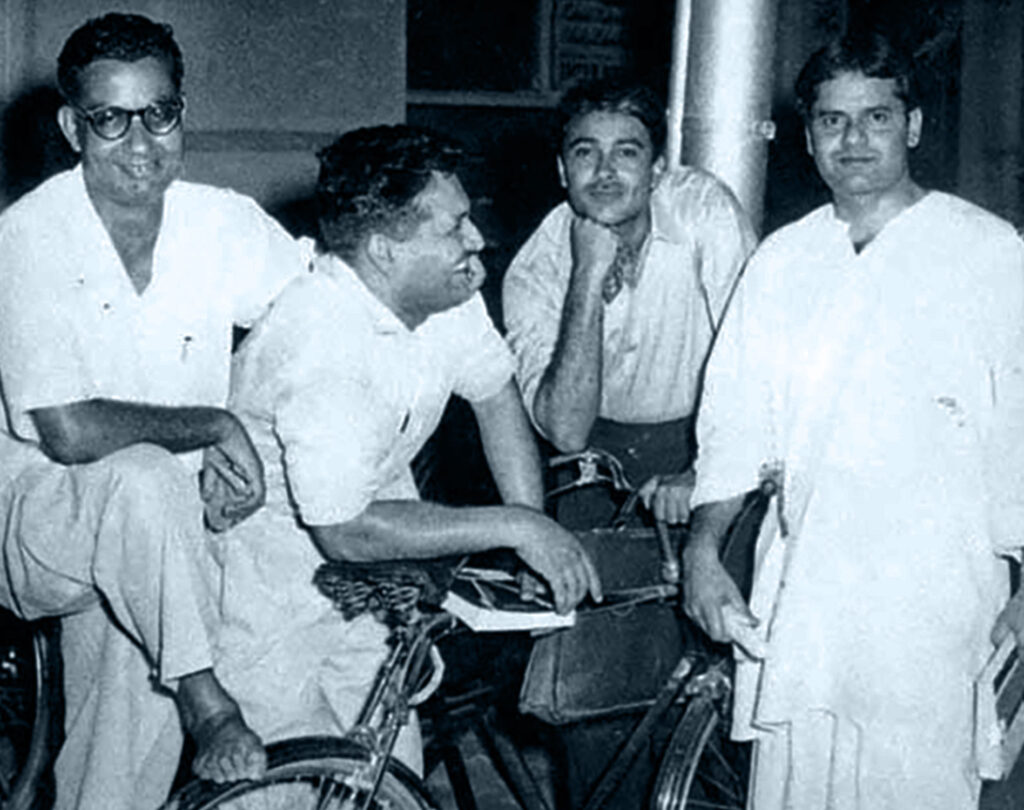
इस एक शेर में मीर के दो अशआर की झलक-सी देखी जा सकती है। वो दोनों शेर हैं :
गुल हो, महताब हो, आईना हो, ख़ुर्शीद हो मीर
अपना महबूब वही है जो अदा रखता हो
और,
हम फ़क़ीरों से बे-अदाई क्या
आन बैठे जो तुमने प्यार किया
जब मीर, इब्न-ए-इंशा और चाँद का अज़कार एक साथ कर रहा हूँ तो ऐसा गुमाँ गुज़रने लगता है कि एक छोटे से हल्क़ा-ए-अहबाब के हवाले से बात हो रही है, जिसमें एक को दूसरे से गहरी निस्बत रही है। चाँद के हवाले से इब्न-ए-इंशा के कुछ शेर देखें :
साँझ समय कुछ तारे निकले, पल-भर चमके डूब गए
अंबर-अंबर ढूँढ रहा है अब उन्हें माह-ए-तमाम कहाँ
तू भी हरे दरीचे-वाली, आ जा बर-सर-ए-आम है चाँद
हर कोई जग में ख़ुद सा ढूँढे, तुझ बिन बे-आराम है चाँद
चाँद से निस्बत इस दर्जा है कि उन्होंने अपने एक मजमूआ-ए-कलाम का नाम भी ‘चाँद-नगर‘ रखा था। चाँद के तअल्लुक़ से उन्होंने नज़्में भी कही हैं। उनकी एक नज़्म भी मुझे बेहद पसंद है, जिसका उन्वान ‘चाँद के तमन्नाई’ है। इब्न-ए-इंशा की शायरी की तासीर भी चाँदनी की सी महसूस होती है – नर्म, उजली, ख़ुनक और शफ़्फ़ाफ़। उनका उस्लूब उर्दू ग़ज़ल में उनकी ईजाद ही नज़र आता है।

उनकी ग़ज़लों में चंद अल्फ़ाज़ को उन्होंने इस तरह बरता है जिससे अवधी और ब्रज के भक्ति काव्य का असर उस कलाम पर साफ़ नज़र आता है। मसलन “अब मन का उजाला सँवलाया, फिर शाम है मन के आँगन में“। ‘साँवला होने’ की जगह ‘सँवलाना’ बरतना इस बात की ताईद करता है। सँवलाया लफ़्ज़ जिस ख़ूबी से इस शेर में इस्तिमाल हुआ है, उससे इस शेर में एक मुख़्तलिफ़ नौइयत की मिठास पैदा हो गई है। इसकी दूसरी मिसाल यह शेर हो सकता है :
हम साँझ समय की छाया हैं, तुम चढ़ती रात के चंदरमा
हम जाते हैं, तुम आते हो, फिर मेल की सूरत क्योंकर हो
‘चंदरमा’ लफ़्ज़ का इस्तिमाल उससे इस शेर में एक मुख़्तलिफ़ नौइयत की मिठास पैदा हो गई है, जिससे इस शेर पर लोकगीत होने का गुमाँ गुज़रने लगता है। इस से हट कर उनके अशआर में जिन इस्तिआरात का इस्तिमाल हुआ है, वो हिंदुस्तानी तहज़ीब से जुड़े हुए नज़र आते हैं। मसलन ये शेर :
कुछ मन के अजंता में आओ, वह मूरतें तुमको दिखलाएँ
वह सूरतें तुमको दिखलाएँ, हम खो गए जिनके दर्शन में
या बन में चिकारे मिलते हैं, या पीत के मारे मिलते हैं
कुछ पूरब में, कुछ पच्छम में, कुछ उत्तर में, कुछ दक्खन में
एक तरफ़ इब्न-ए-इंशा अपनी शायरी में मर्तबा-ए-कमाल तक पहुँचे। ‘कल चौदहवीं की रात थी’ और ‘इंशा-जी उठो अब कूच करो’ दोनों मशहूर-ए-ज़माना ग़ज़लें हैं। ‘फ़र्ज़ करो’ और ‘इस बस्ती के इक कूचे में’ जैसी नज़्में हर शायरी का ज़ौक़ रखने वाले की ज़बान पर हैं। दूसरी तरफ़ उन्होंने उर्दू तंज़-ओ-मज़ाह में भी कई कार-हा-ए-नुमायाँ अंजाम दिए। ‘उर्दू की आख़िरी किताब’ अब भी उर्दू की तंज़िया तस्नीफ़ात में अपना मक़ाम रखती है। ‘कस्टम का मुशायरा’ और दीगर मज़ामीन अभी भी उसी तरह पढ़े जाते हैं और उतनी ही मुताबिक़त रखते हैं जितनी अपने शाया होने के वक़्त रखते थे। कॉलम-निगार की हैसियत से भी इब्न-ए-इंशा का नाम खासी अहमियत रखता है। उन्होंने बहुत सारे मग़रिबी मुल्कों में सफ़र किया और सफ़रनामे की सिन्फ़ में भी उनकी तख़्लीक़ात भी क़ाबिल-ए-ग़ौर हैं। उनका इन्तिक़ाल भी आज ही दिन (11 जनवरी), 1960 में लंदन के एक अस्पताल में हुआ, जिस की वज्ह उनका कैंसर बना। बाद में उनकी मौत के बारे में एक क़िस्सा मशहूर हो गया।

उनकी एक ग़ज़ल ‘इंशा-जी उठो अब कूच करो’ को जब उस्ताद अमानत अली ख़ान ने गाया तो ये ग़ज़ल मक़बूलियत की इंतिहा पर पहुँच गई और इसे बेहद पसंद किया गया, लेकिन चंद महीनों बाद उनकी मौत हो गई। उनके बेटे असद अमानत अली ने भी जब ये ग़ज़ल गाई तो ये ग़ज़ल उनकी आख़िरी ग़ज़ल बन गई। इब्न-ए-इंशा ने अस्पताल में ही अपने एक दोस्त को ख़त लिख कर कहा था कि “ये मनहूस ग़ज़ल और कितनों की जान लेगी।” ये ख़त लिखने के अगले दिन उनका इन्तिक़ाल हो गया। हालाँकि इस ग़ज़ल को बहुत लोगों ने आवाज़ दी है। इस बात को संजोग और वहम ही कहा जा सकता है। लेकिन इंशा-जी ख़ुद कह गए हैं :
जब शहर के लोग न रस्ता दें क्यूँ बन में न जा बिसराम करे
दीवानों की सी न बात करे तो और करे दीवाना क्या
NEWSLETTER
Enter your email address to follow this blog and receive notification of new posts.




