
यहाँ बैठ कर शिकायतें भी होती थीं और मोहब्बतें भी
माया-नगरी मुंबई जैसे एक कोह-ए-निदा है, जो हर वक़्त आवाज़ देता रहता है और लोग-बाग बोरिया-बिस्तर बांधे जूक़ दर जूक़ इसकी तरफ़ भागे चले आते हैं। इस शहर के आकर्षण में समुंदर के अलावा दो और चीजों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक तो ये देश की आर्थिक राजधानी है और दूसरे यहाँ बॉलीवुड नाम की एक परी रहती है, जिसने सबको अपने जादू में गिरफ़्तार कर रखा है। रोज़ हज़ारों नौजवान अपने अपने गाँव और शहरों से हीरो बनने की आस में इस जादू नगरी का रुख़ करते हैं। उनमें से कुछ तो अपने मन की मुराद पा जाते हैं लेकिन ज़्यादा तर एक्स्ट्रा की शक्ल में अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ार देते हैं।
शायरों और अदीबों पर अलबत्ता फ़िल्म इंडस्ट्री के दरवाज़े हमेशा खुले रहे। 60 और 70 के दशक में तो ये हाल था कि हर क़ाबिल-ए-ज़िक्र शाएर और अदीब ने फ़िल्मों का दामन थामा। उसकी एक वजह तो ये थी कि फ़िल्मों से अच्छी-ख़ासी कमाई हो जाती थी। दूसरे उन दिनों बम्बई तरक़्क़ी-पसंद तहरीक का एक बड़ा मरकज़ था। जो शायर और अदीब यहाँ आए वो सब इस तहरीक के पुर-जोश सिपाही थे। शायरों और अदीबों की क्या बात करें, उस ज़माने के बहुत सारे ऐक्टर तक इस तहरीक से वाबस्ता थे। बलराज साहनी से जुड़ा हुआ का एक बड़ा दिलचस्प क़िस्सा है कि एक बार वो अपने विचारों की वजह से जेल में बंद थे तो उन्हें रोज़ाना शूटिंग के लिए सुबह जेल से लाया जाता और शाम को वापस उनके बैरक में पहुँचा दिया जाता। मजरूह साहेब को अपनी एक नज़्म जिसमें उन्होंने ये बंद बांधा है ”मार ले साथी जाने ना पाए” एक मुशायरे में पढ़ने के बाद कई महीनो तक अंडर्ग्राउंड रहना पड़ा।
शायरों और अदीबों के इस जमावड़े ने जहां जहाँ फ़िल्मी दुनिया में चार चाँद लगाए, वहीं बम्बई के अदबी और संस्कृतिक माहौल को भी ख़ूब गरमाया। शब-बाशियों के साथ साथ सुबह और शाम के औक़ात में कुछ मख़्सूस होटलों में महफ़िलें जमतीं जहाँ शेर-ओ-शायरी भी होती, अफ़साने भी सुनाए जाते, और एक दूसरे की टांग भी खींची जाती। आज हम आपका तआरुफ़ कुछ ऐसी ही जगहों से कराते हैं।
होटेल सारवी 60 और 70 की दहाई में उर्दू के ज़्यादा तर अदीब और शाएर भिंडी बाज़ार, नागपाड़ा और मदनपुरा के अत्राफ़ में रहते थे। और बैठक जमाने के लिए या तो ‘मक्तबा जामिया’ था या ‘सारवी होटेल’ में बैठते थे। ‘मक्तबा जामिया’ में लम्बी गप-शाप लगाई नहीं जा सकती थी इसलिए ‘होटेल सारवी’ उनकी पसंदीदा जगह थी (एक दूसरा होटेल ‘होटेल वज़ीर’ भी था, लेकिन ज़्यादा लोगों की पसंद सारवी था) ये वो ज़माना था जब इन शायरों और अदीबों पर दौलत के दरवाज़े पूरी तरह नहीं खुले हुए थे और इस तरह के सस्ते लेकिन मेयारी होटेल और रेस्तराँ ही उनकी जेब सहार सकती थी। बाद में कैफ़ी जानकी कुटीर चले गए। साहिर ने बांद्रा में शानदार बंगला ख़रीद लिया, सरदार जाफ़री ने पेडर रोड पर एक महँगा फ़्लैट ख़रीद लिया। मजरूह भी एक पॉश जगह मुंतक़िल हो गए, लेकिन ये बात उस जमाने की हो रही है जब ये सब लोग एक तरह से स्ट्रगल कर रहे थे। सारवी का मालिक भी अदबी ज़ौक़ रखता था और ये बैठकें उसे भी बहुत पसंद थीं।
इन शायरों ने तो इस बम्बई की तस्वीर-कशी नहीं की है लेकिन मंटो ने अपने बहुत सारे अफ़सानों और कहानियों में इन जगहों का ज़िक्र किया है। हमें ‘सारवी होटेल’ भी दिखाई देता है, कमाठीपुरा की गालियाँ भी हैं (मंटो ने अपनी बहुत सारी कहानियाँ का ताना-बाना कमाठीपुरा से बुना है, ये तवैफओं का इलाक़ा है) एक दिलचस्प बात ये है की जब मैं बम्बई आया तो कितने सालों तक ‘बोरी बंदर’ ढूँढता रहा (मंटो की कई कहानियों में बोरी बंदर का ज़िक्र मिलता है) बाद में किसी ने बताया की विक्टोरिया टर्मिनल्स के आस-पास का इलाक़ा ‘बोरी बंदर’ के नाम से जाना जाता था।
Pamposh: बांद्रा लिंकिंग रोड पर वाक़े Pamposh एक ज़माने में बैठक-बाज़ी का बहुत बड़ा अड्डा था। अब यहाँ पर ‘कैफ़े कॉफ़ी डे’ आ गया है। हमारे करम-फ़रमा और उर्दू के एक बड़े सिपाही ज़मील गुलरेज़ साहेब अपनी याददाश्तों से इस जगह से जुड़ी एक बड़ी ख़ूबसूरत कहानी लाए हैं (ज़मील साहेब कथा-कथन के नाम से भारती भाषाओं को बचाने की एक मुहिम चला रहे हैं) ये उन दिनो की बात है जब जावेद अख़्तर, निदा फ़ाज़ली, जावेद सिद्दीक़ी, और अनजान जैसे लोगों का यहाँ पर उठना-बैठना होता था। ज़मील साहेब भी इस ग्रूप का हिस्सा थे। ये सारे लोग अभी पूरी तरह इस्टैब्लिश नहीं हुए थे इसलिए Pamposh जैसी जगहें ही ठिकाना थीं। निदा साहेब की अक्सर उनके इस शेर की वजह से खिंचाई हो जाती थी।
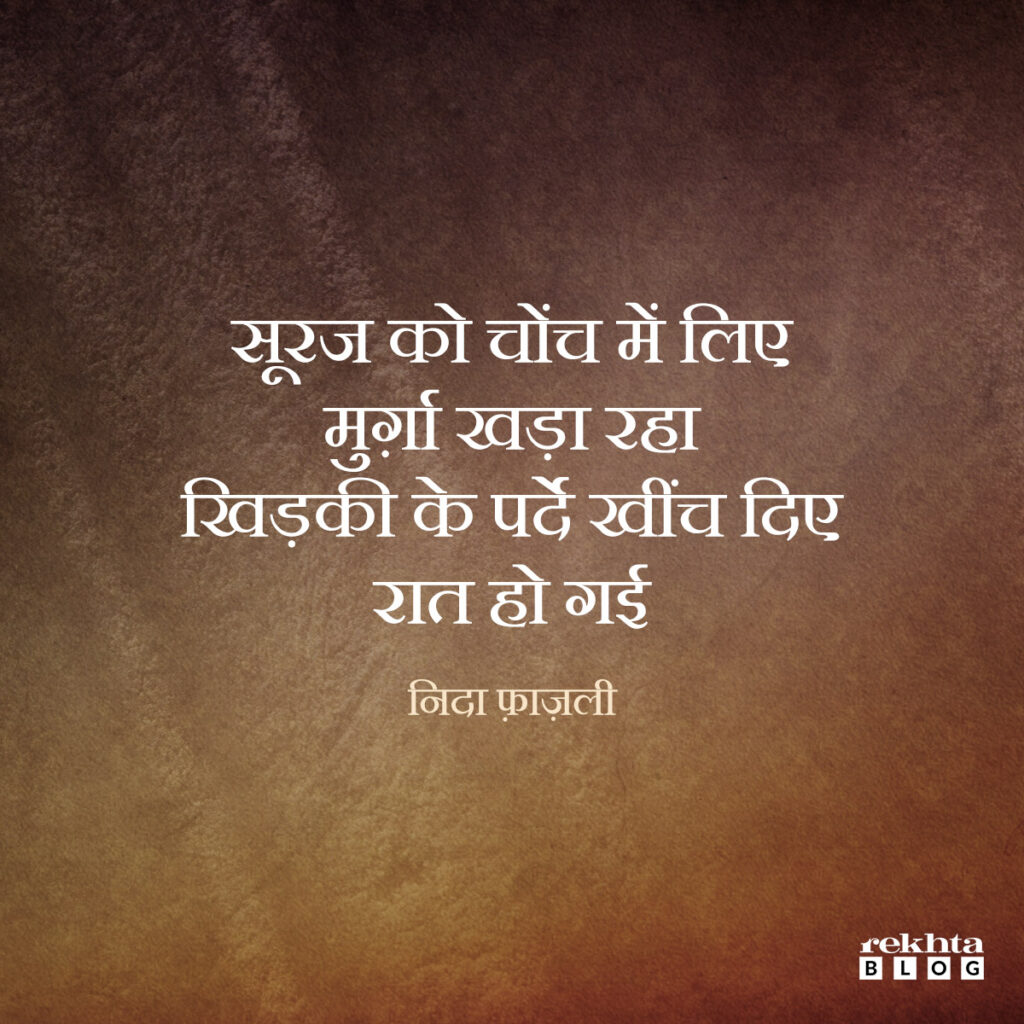
ज़मील साहेब की मानें तो निदा साहेब की शायरी उन दिनो शरीफ़ घरानो में ममनूअ’ थी कि उन्होंने एक Sensuous नज़्म लिख दी थी। नज़्म कुछ इस तरह है:
गाँव लौटे कई बरस बीते
वो चँबेली सी बढ़ रही होगी
पोल्का और कस गया होगा
ओढ़नी छोटी पड़ गई होगी
Pamposh का क़िस्सा नसीरुद्दीन शाह ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी ‘’और फिर एक दिन’’ में बयान किया है कि वो 16 साल की उम्र में घर से ऐक्टर बनने के लिए भाग आए थे, और जब घर वालों को पता चला तो दिलीप कुमार साहेब की फ़ैमिली को, जिनसे उनके घरेलो तअ’ल्लुक़ात थे, उनको ढूँढने और घर वापस भेजने का फ़र्ज़ सौंपा गया। नसीर साहिब के अल्फ़ाज़ में ‘’एक सुबह एक बड़ी सी गाड़ी से दो ख़ूबसूरत पैर निकलते हैं, जो उनकी तरफ़ चले आ रहे हैं’’ ये दिलीप साहेब की बहन सईदा बानो थीं जो उन्हें घर ले जाती हैं जहाँ दिलीप साहेब उनको लेक्चर देते हैं कि शरीफ़ घराने के बच्चे फ़िल्मों में काम नहीं करते हैं। नसीर साहेब का उन दिनों Pamposh की चाय और खाने पर गुज़ारा था, सामने फ़ुट्पाथ पर दिन भर बैठे रहते और सोने के लिए रात में पड़ोस के पार्क में चले जाते थे।
Pamposh के सामने बांद्रा नैशनल कॉलेज है जहाँ अमजद ख़ान पढ़ते थे और कई साल से इसलिए फ़ेल हो रहे थे कि अगर पास हो गए तो यहाँ से जाना पड़ेगा और वो फिर थेटर नहीं कर पाएँगे। Pamposh ने न जाने कितने लोगों को स्ट्रगल और फिर स्टार बनते देखा होगा।
मालवानी: मालवानी का इलाक़ा भी उर्दू का अहम मरकज़ रहा है। जगजीत सिंह की आवाज़ में गाई हुई ये नज़्म ‘बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी’ पूरी दुनिया में धूम मचा चुकी है, लेकिन इसकी बद-क़िस्मती की शायर कफ़ील आज़र को कम लोग ही जानते हैं। जगजीत सिंह ने हमेशा स्टेज पर नाम लिया है, कैसेट पर भी नाम लिखा है लेकिन कफ़ील फिर भी गुमनामी के पर्दे में छुपे रहे। न उनके हालात-ए-ज़िंदगी का पता है न बूद-ओ-बाश का, और सबसे बड़ी बदक़िस्मती तो ये है कि कलाम का भी पता नहीं। ये बाँका सजीला शायर इसी मालवानी की बस्ती में रहता था। बस हमारी मालूमात इतनी ही है।
नवा लखनवी नाम के भी एक शायर गुजरे हैं जिन्हो ने मालवानी को अपना मसकन बनाया था। उनका एक ख़ूबसूरत शेर मुलाहिज़ा फ़रमाएँ:
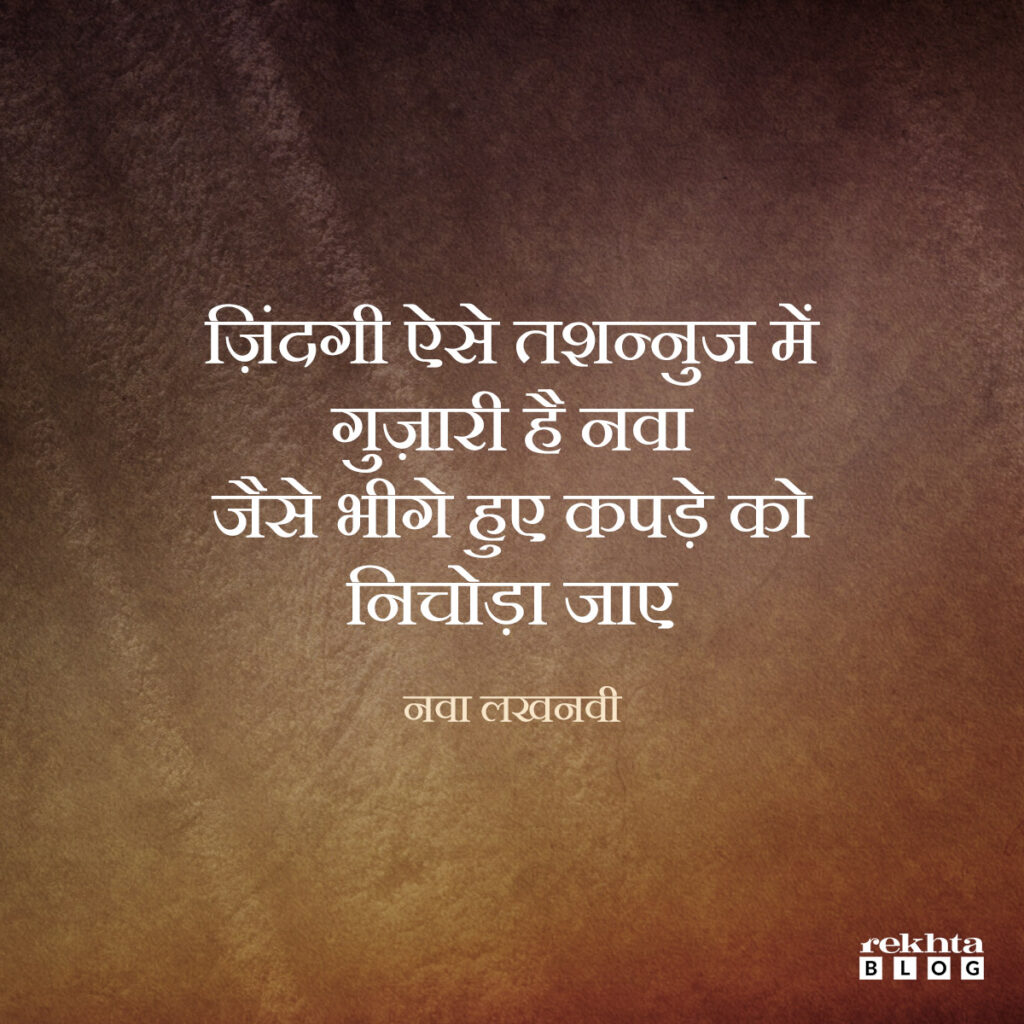
और भी कई शायर और अदीब यहाँ मकीन थे। फिर 90 का दशक आते आते उर्दू की ये बस्ती उजड़ गई। इसके बाद कुर्ला, मुम्ब्रा और दूसरे मज़ाफ़ात में उर्दू की बस्तियाँ बसना शुरू हुईं, लेकिन वो पहली सी बात नहीं रही। उसका एक सबब तो ये था कि शायरों और अदीबों की वो खेप जिसने बम्बई की अदबी सरगर्मियों में अपने रंग बिखेरे थे, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। बाक़ी रहे जावेद अख़्तर और गुलज़ार साहिब जैसे लोग तो उनके लिए उन अवामी मुक़ामात पर बैठना मुमकिन नहीं रहा। रही नए शायरों और अदीबों की नस्ल तो वो अभी अपना मुक़ाम ढूँढ रही है। यकीनन वो भी अपनी महफ़िलें जमाते होंगे लेकिन अभी उनमें कोई इतनी तवाना आवाज़ नहीं कि उसका चर्चा हो।
एक ज़माना था कि हर क़ाबिल-ए-ज़िक्र अदीब और शायर बम्बई को अपना मस्कन बनाता था कि शोहरत और दौलत दोनो पाने का इम्कान था। लेकिन न अब वो जौहर-शनास रह गए और न ही वो हीरे। फ़िल्मी दुनिया के गिरते मेयार और वेब सिरीज़ के इस दौर में वो होते भी तो क्या कर लेते। अब न ओ पी नय्यर जैसे मौसीक़ार हैं, जो ‘अनजान’ को कह सकें कि आप का कलाम मैं ने देखा है। आप हिंदी के शब्द ज़ियादा इस्तेमाल करते हैं, और मुझे गाने में उर्दू के अल्फ़ाज़ चाहिएँ। और न ही यश चौपड़ा जैसा बड़ा Director जो बर्मला कहता था कि साहिर जैसा शायर फिर फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं आया। अब ये सारी बातें गुज़रे ज़माने की हैं। वैसे हमें हालात का रोना नहीं रोना चाहिए कि प्रकीर्ति का नियम यही है। अंग्रेज़ी की एक कहावत है कि All good things come to an end तो शाएद अब हम न बम्बई की वो अदबी महफ़िलें देखेंगे जिसने अदब को एक नए मुक़ाम पर पहुँचाया था और न ही वो बैठकें जिसने ये सिखाया था कि ज़िंदगी को कैसे बरता जाए।
NEWSLETTER
Enter your email address to follow this blog and receive notification of new posts.




