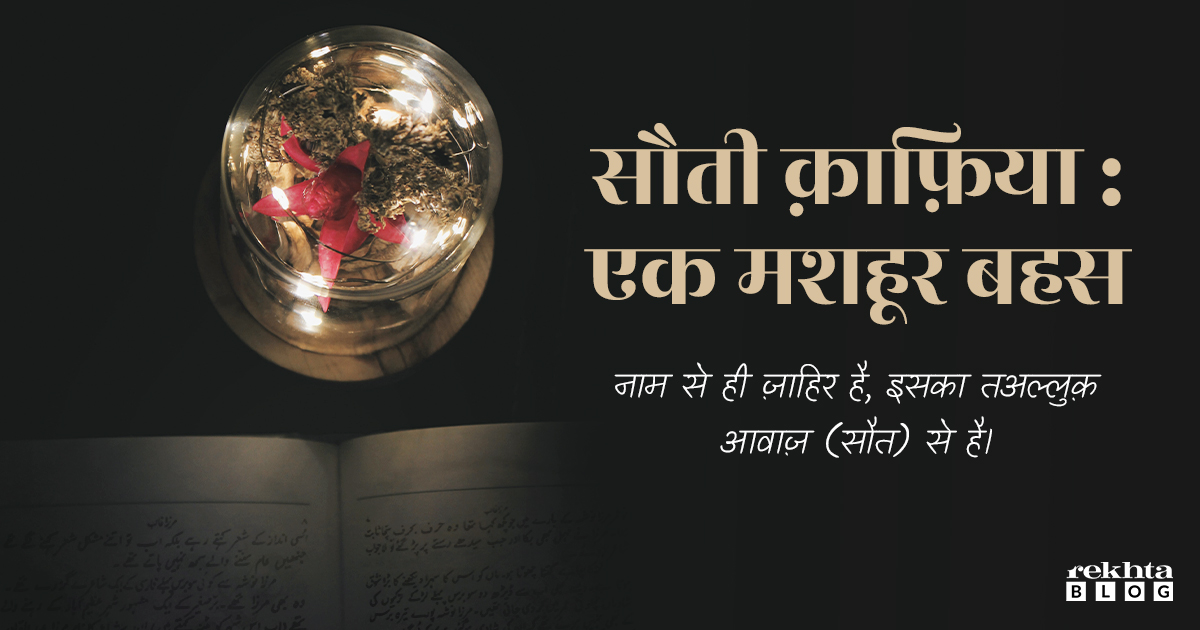
क़ाफ़िये की ये बहसें काफ़ी दिलचस्प हैं
अक्सर एक इस्तिलाह (term) सुनने में आती है सौती क़ाफ़िया। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, इसका तअल्लुक़ आवाज़(सौत) से है।
इस बात से कौन इंकार कर सकता है की ग़ज़ल का फ़ॉर्मेट मौसीक़ियत (musicality) पर मब्नी है, रदीफ़: – या’नी एक ही लफ़्ज़ का कान में बार बार तकरार, क़ाफ़िया: – या’नी एक जैसी आवाज़ का बार बार आना, बहर: – या’नी हर शे’र एक रिद्म, एक ताल पर कसा हुआ, इस सबका तअ’ल्लुक़ ज़ाहिर है कि सुनने से है, आवाज़ से है, और नग़्मगी से है।
सौती क़ाफ़िया या’नी लफ़्ज़ सुनने में एक जैसी आवाज़ देते हों चाहे उनका इमला (spelling) अलग हो। मसलन ख़त के आख़िर में ‘तोय’(خط) है और मत(مت) के आख़िर में ‘ते’ है तो देखने में बे-शक ये एक दूसरे से मुख़्तलिफ़ मा’लूम होते हैं मगर सुनने में एक ही आवाज़ देते हैं। इसी तरह ‘ख़ास’ और ‘पास’ का हम-क़ाफ़िया होना। यही सौती क़ाफ़िया है।
बाज़ हज़रात इसे जाएज़ नहीं मानते बाज़ लोग जाएज़ मानते हैं।
जो इसके ख़िलाफ़ हैं उनका कहना है कि चूँकि ग़ज़ल का हुस्न उसकी तहरीरी (written) सूरत भी है इस लिए हर्फ़-ए-रवी का बदलना क़तअन जाएज़ नहीं। या’नी आसान लफ़्ज़ों में समझें तो क़ाफ़िए के वो आख़िरी हर्फ़ जिनकी वजह से क़ाफ़िए एक दूसरे से राइम करते हैं और हम-आवाज़ होते हैं उनका बदलना जाएज़ नहीं।
एक दलील ये भी दी जाती है कि ये ग़ज़ल के असली फ़ॉर्मेट के साथ छेड़-छाड़ है और बे-जा आज़ादी है। सहल-पसंदी की वजह से इसे आम किया जा रहा है।
मैं सौती क़ाफ़िए को जाएज़ मानता हूँ।
क्यूँ मानता हूँ इसके लिए थोड़ा सियाक़-ओ-सबाक़ और थोड़ी सी तारीख़ और मुशाहिदा दरकार है।
अरबी अरूज़ में ऐसी कोई इस्तिलाह मौजूद नहीं थी, उर्दू अरूज़ चूँकि अरबी और फ़ारसी अरूज़ से ही लिया गया है तो आप कह सकते हैं कि ये दलील इस बात को और तक़्वियत (मज़बूती) देती है की उर्दू में भी नहीं होनी चहिए ये।
लेकिन ऐसा है नहीं। अरबी में इस टर्म के न होने की वजह उसूल की सख़्ती नहीं है बल्कि ये है कि वहाँ ‘तोए’ और ‘ते’ का तलफ़्फ़ुज़ अलग है, ‘सीन’, ‘से’ और ‘साद’ का तलफ़्फ़ुज़ अलग है, ऐसे ही ‘ज़े’ ‘ज़वाद’ ‘ज़ोए’ और ‘ज़ाल’ का तलफ़्फ़ुज़ अलग है, उर्दू में ऐसा नहीं है। हमारे इलाक़े में ‘से’ की आवाज़ का एक ही मख़रज है, एक ही तलफ़्फ़ुज़ है, और यही हाल ‘ते’ ‘ज़े’ का भी है।
अरबी में बहुत मुश्किल है कि आख़िरी हर्फ़ बदले और आवाज़ न बदले, तो सौती क़ाफ़िया वजूद ही नहीं रखता वहाँ।
अंग्रेज़ी अदब में भी एक इस्तिलाह है ”visual rhyme” या “eye rhyme” की। या’नी रायमिंग अल्फ़ाज़ में स्पेलिंग के ए’तिबार से मुताबक़त हो, मगर तलफ़्फ़ुज़ (Pronunciation) के ए’तिबार से नहीं, मसलन ‘लव’ और ‘रिमूव’ को एक पोयम में राइम के तौर पर इस्ति’माल करना, इसकी मिसालें ख़ूब मिलती हैं पंद्रहवीं सदी से पहले की पोयम में। हमारे यहाँ जो सौती क़ाफ़िए के मुख़ालिफ़ हैं वो इस से दलील पकड़ सकते हैं कि देखिए अंग्रेज़ी अदब में भी यही रिवाज रहा है कि लफ़्ज़ दिख कैसा रहा है उसका ए’तिबार हो रहा है क़ाफ़िए में और कैसा बोला जा रहा है उसका नहीं। अस्ल में ऐसा है नहीं, ये जो आई रायम की इस्तिलाह है ये उस वक़्त मौजूद ही नहीं थी, वजह ये थी कि उस वक़्त ‘लव’ और ‘रिमूव’ एक ही तरह बोले जाते थे, बा’द में जब अंग्रेज़ी अल्फ़ाज़ के तलफ़्फ़ुज़ में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए तब ये तलफ़्फ़ुज़ बदले। उस दौर को ‘‘great vowel shift’’ भी कहा जाता है।
या’नी अस्ल वहाँ भी लफ़्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ था, स्पेलिंग नहीं।
और ये मसअला हर उस ज़बान के साथ है जिसकी स्क्रिप्ट पूरी तरह फ़ोनेटिक नहीं होती या’नी, सौतियत या आवाज़ पर मब्नी नहीं होती। उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी और फ्रेंच में भी ये प्रॉब्लम है कि बहुत से लफ़्ज़ हैं जो एक जैसी आवाज़ देते हैं, लेकिन स्पेलिंग के ए’तिबार से वो अलग हैं। लेकिन फ्रेंच में और इंग्लिश में रायम की बुनियाद आवाज़ ही है, ‘टफ़’ और ‘कफ़’ अंग्रेज़ी में हम-क़ाफ़िया हैं, और eye rhyme (या’नी स्पेलिंग एक जैसी लेकिन तलफ़्फ़ुज़ अलग) या तो किसी भी ज़बान में जाएज़ नहीं है, और अगर है भी तो इस्तिस्ना (exception) के तौर पर। मेरा ख़याल है कि किसी और ज़बान की शायरी में ये इस्तिलाह सौती क़ाफ़िए की है ही नहीं, इंग्लिश में शायद कोई वर्ड नहीं है इस सूरत के लिए कि जब दो लफ़्ज़ राइम कर रहे हों, मगर स्पेलिंग अलग हो। क्यूँकि मा’लूम है कि पोयम में रायम का मक़्सद नग़मगी म्यूज़िकल्टी है और उसका तअल्लुक़ आवाज़ से है, न कि स्पेलिंग से।
उर्दू के साथ मसअ’ला ये हुआ जो अक्सर ज़बानों के साथ नहीं है, कि एक ही आवाज़ के लिए तीन-तीन चार-चार हर्फ़ हैं इसमें। मैं अभी आप से अगर पूछूँ कि ‘स’ आवाज़ के लिए देवनागरी में क्या हर्फ़ है तो आप फ़ौरन एक ही हर्फ़ बताएँगे। लेकिन यही उर्दू के लिए पूछूँ तो आपके पास तीन हर्फ़ हैं। ये इस स्क्रिप्ट की प्रॉब्लम है। और इसकी वजह ये है कि हमने जिस ज़बान से ये स्क्रिप्ट ली है उनकी ज़बान की आवाज़ें हमारे यहाँ थीं नहीं, तो उनके यहाँ जो चार आवाज़ें थीं हमारे यहाँ वो एक ही है। लेकिन हर्फ़ लेने पड़े। हालाँकि ये भी माँग होती रही है कि स्क्रिप्ट में रिफ़ार्म किए जाएँ और एक आवाज़ के लिए एक ही हर्फ़ का तअ’य्युन किया जाए। लेकिन ये इस लिए भी मुम्किन नहीं की हमारी vocabulary का बेशतर हिस्सा अरबी अल्फ़ाज़ पर मुश्तमिल है और एक आवाज़ के लिए एक हर्फ़ वज़्अ करने की वजह से एक लफ़्ज़ के तमाम फ़ार्मस बदलेंगे और इश्तिबाह और कंफ्यूज़न फैल जाएगा। या इम्ला बदलने से किसी और लफ़्ज़ का धोका हो सकता है। मसलन शरारतन ((شرارتاً पर तनवीन है या’नी दो ज़बर, जो हाल और तौर के मा’नी के लिए आती है (उर्दू में) या’नी शरारत के तौर पर। अगर तनवीन की जगह शरारतन के आख़िर में नून लगा दिया जाए (شرارتن) तो ये कंफ्यूज़न हो सकता है की ये दो लफ़्ज़ हैं, एक शरार और एक हिंदी वाला ‘तन’ या’नी जिस्म है। इन्हीं कुछ मजबूरियों की वजह से जो रिफ़ार्मस हो सकते थे वो न हो पाए।
या’नी ये जो अदम मुताबक़त है स्क्रिप्ट और सौतियत में, ये ज़रूरी भी है इस वजह से कि हमारी वोकैबुलरी का बहुत बड़ा हिस्सा अरबी फ़ारसी से आया है और ये परेशानी का सबब भी है कि एक आवाज़ के लिए 4 या 3 हर्फ़ मौजूद हैं।
किसी भी ज़बान में हर्फ़ सबसे छोटी इकाई होता है और हर्फ़ या लेटर की तारीफ़ (definition) है “a character or symbol which represents a specific sound used in speech” या’नी हर्फ़ वो इकाई या अलामत है जो किसी भी ज़बान की एक ख़ास आवाज़ की नुमाइंदागी करता है। ज़बान के जितने भी रिफ़ार्मस हुए हैं किसी भी ज़बान में, चाहे वो इमला के हवाले से हों या तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से हों, सब की बुनियाद सुहूलत रही है। सुहूलत कोई मा’यूब चीज़ नहीं है मगर मंतिक़ी दलाइल (logical arguments) की बिना पर ली जाए।
इंगलिश में बहुत स्पेलिंग रिफ़ार्मस हुए हैं, मसलन error पहले errour था music musick था।
इमला(spelling) और तलफ़्फ़ुज़ (pronunciation) में यकसानियत न होने का मज़ाक उड़ाते हुए एक स्पेलिंग अज़-राह-ए-तंज़ मशहूर की गई थी, जिससे लोगों का ध्यान जाए कि एक आवाज़ के लिए अलग अलग हर्फ़ होने में क्या परेशानी हो सकती है। ये Fish की स्पेलिंग थी जिसे घोटी (GHOTI) लिखा गया था। कहा था कि क्योंकि rough के आख़िर में f आवाज़ GH से ज़ाहिर हो रही है तो Fish में ‘F’ की जगह GH. लगाया, वुमेन women (का तलफ़्फ़ुज़ विमेन) wimen होता है या’नी आई ( i ) की आवाज़ को ओ (o) से ज़ाहिर किया है तो फ़िश में आई (i) की जगह (o) लगाया, मेन्शन (mention) में श. आवाज़ के लिए टी.आई TI है तो फ़िश में श आवाज़ के लिए TI लगाया और फ़िश का इमला घोटी “ghoti” बनाया।
बहर-हाल, हर्फ़ की बुनियाद भी सौत पर ही है या’नी स्क्रिप्ट ख़ुद आवाज की नुमाइंदा भर है। ज़बान में अस्ल आवाज़ है। तो ग़ज़ल जैसी सिंफ़, कि जिसमें ज़बान सिर्फ़ इज़हार-ए-ख़याल के लिए ही नहीं बल्कि मौसीक़ी और नग़्मगी भी उसके फ़ार्मेट का लाज़मी हिस्सा है, उसमें सौती क़ाफ़िए से इंकार की मंतिक़ समझ से बाहर है, हाँ अगर उर्दू में ‘ज़ुआद’ ‘ज़ोए ‘ज़ाल’ ज़े की अलग आवाज़ होतीं तो बात अलग थी। सिर्फ़ तहरीरी शक्ल (written form) और साख़्त की वजह से इसे रद्द करना समझ से बाहर है जब-कि तहरीर ख़ुद आवाज़ के सिंबल से ज़ियादा कुछ हैसियत नहीं रखती, सिंबल को अस्ल पर तरजीह (preferrence) देना कहाँ दुरुस्त है?
इमला नहीं बदला जा सकता तो वो मजबूरी है, लेकिन उस मजबूरी को दलील बना कर ये कहना कि क़ाफ़िए में ऐसा नहीं किया जा सकता ये इस लिए दुरुस्त नहीं कि ख़ुद जो सौती क़ाफ़िए की मुख़ालिफ़त करते हैं वो ज़ालिम को ज़्वौलिम नहीं बोलते, ज़मीर को ‘धमीर’ नहीं बोलते। या’नी ख़ुद भी मानते हैं की ज़े और ज़ुआद के हर्फ़ की उर्दू में एक ही आवाज़ है। और एक आवाज़ के लिए इतने हर्फ़ होना ज़बान की कमी है, तो कमी को दलील बनाना कैसे दुरूस्त हुआ?
एक बात और याद आई जिसका इस बहस से ख़ास तअ’ल्लुक नहीं, हाँ अरबी और उर्दू के इख़्तिलाफ़ के हवाले से है। अरबी में जुमले में जब लफ़्ज़ इस्ति’माल होता है तो आख़िरी हर्फ़ पर ए’राब या’नी ज़बर, ज़ेर, पेश, अक्सर होता है, जो ये तय करता है कि इस लफ़्ज़ की सेंटेन्स में हैसियत क्या है, क्या ये सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट। तो वहाँ आप को अगर लफ़्ज़ शम्अ’ (شمع) मिलेगा तो अक्सर आख़िर का ऐन वहाँ साकिन नहीं होगा बल्कि उस पे ज़बर, ज़ेर, पेश, के ज़रिए एक अ, ई, या यू की आवाज़ होगी। या’नी शम्अ’ या शम्ई’ या शम्उन या शम्अन। एक तो उर्दू के फ़ोनीमी निज़ाम में ऐन की आवाज़ नहीं, फिर उस पे शम्अ का ऐन साकिन भी है, उर्दू में तो मजबूर होकर हमें शम्अ’ बर-वज़न हुमा या शम्म्अ’ बोलना पड़ता है और ज़ियादा जानने वाला शम्म पर इक्तिफ़ा करता है।
यही हाल ऐसे और लफ़्ज़ों का है जिनकी अस्ल अरबी है और उनमें आख़िर के दो हर्फ़ साकिन हों और उर्दू ज़बान के इलाक़े में ऐसे अल्फ़ाज का चलन न रहा हो। मसलन ज़बर तो बोल लेंगे मगर नफ़अ’ (نفع) नहीं बोल पाएँगे। या तो ‘नफ़ा’ बोलेंगे। ‘ऐन’ वैसे ही नहीं निकलता, यहाँ तो ‘ऐन’ के आगे पीछे कोई सपोर्टिंग आवाज़ भी नहीं है।
बहर-हाल ये मसअले ज़िद के नहीं होते, ना ही ये ऐसे होते हैं कि इन पर बात करने से ‘‘ग़ज़ल की आबरु मजरूह’’ हो जाती है। ग़ज़ल की आबरू उस चीज़ से कैसे मजरूह हो सकती है जो न आहंग के ख़िलाफ़ न नग़्मगी के ख़िलाफ?
इसी के बर-ख़िलाफ़ मिसाल देखिए। ग़ालिब की ग़ज़ल है जिसका क़ाफ़िया है राज़ी, तसल्ली, भी। और रदीफ़ है ‘‘न हुआ’’ या’नी ‘राज़ी न हुआ’ ‘तसल्ली न हुआ’ ‘भी न हुआ’ अब चूँकि लफ़्ज़ ईसा और तक़्वा के आख़िर में भी ‘ये'(ی) है, (और ये अलिफ़ मक़सूरा है), और मआ’नी, तसल्ली, राज़ी में भी “ये”(ی) है तो ग़ालिब ने यहाँ एक शे’र में ‘‘ईसा न हुआ’’ बाँधा है और एक में तक़्वा न हुआ। ग़ज़ल पढ़ते या सुनते वक़्त जब ये लफ़्ज़ आता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा मा’लूम नहीं देता बल्कि तसलसुल टूट जाता है, ग़ालिब ने उसी उसूल की पैरवी की है कि क़ाफ़िया देखने में एक जैसा लगे। ये अलग बात कि नज़्म तबातबाई ने कहा है कि यहाँ ग़ालिब ने जो ‘ईसा और तक़्वा’ बाँधा है, ये फ़ारसी वालों की इत्तिबा’ की है कि वो लोग अरबी अल्फ़ाज़ जिन के आख़िर में अलिफ़ मक़सूरह होता है उसे कभी अलिफ़ मक़सूरह और कभी ‘ये’ के साथ नज़्म करते हैं या’नी तसल्ली तसल्ला, तमन्नी तमन्ना वग़ैरा।
तो अगर ये मानें कि ग़ालिब ने ईसा बाँधा तो साफ़ ज़ाहिर है कि सौती आहंग का तसलसुल टूटता है, और अगर ये माना जाए कि ग़ालिब ने ईसी बाँधा है तो ये मानना पड़ेगा की ग़ालिब ने मज़मून को तरजीह देने के लिए उर्दू तलफ़्फ़ुज़ से हट कर फ़ारसी वालों की इत्तिबा’ को भी जाएज़ माना और एक ग़ैर-राइज तलफ़्फ़ुज़ को भी नज़्म करने से परहेज़ न किया। हम तो इससे भी बहुत कम पे राज़ी हैं कि उर्दू ही में राइज तलफ़्फ़ुज़ और आवाज़ की बुनियाद पर क़ाफ़िए का तअ’य्युन हो।
ग़ालिब ने अपनी ग़ज़ल (कहते हैं न देंगे हम, दिल मगर पड़ा पाया) जिस में ‘अलिफ़’ का क़ाफ़िया है और रदीफ़ ‘‘पाया’’ है उसके एक शे’र में मज़ा का इमला मीम, ज़े, हे (مزہ) नहीं बल्कि मीम, ज़े, अलिफ़ (مزا) लिखा है। या’नी ‘हे’ और अलिफ़ की वजह से बेशक क़ाफ़िए देखने में मुशाबह (similar) नहीं हैं लेकिन चूँकि अलिफ़ और हा-ए-मुख़्तफ़ी यहाँ आवाज़ में मशाबह हैं, इस लिए ग़ालिब ने इमला ही बदल दिया और अलिफ़ से मज़ा लिखा।
नज़्म तबातबाई ने इस शे’र की तशरीह में लिखा हैः-
शोर-ए-पंद-ए-नासेह ने ज़ख़्म पर नमक छिड़का
आप से कोई पूछे तुम ने क्या मज़ा पाया
‘‘आप का इशारा नासेह की तरफ़ है और इसमें तअ’ज़ीम (respect) निकलती है और मक़्सूद तशनीअ’ है मुसन्निफ़ ने मज़ा को क़ाफ़िया किया और हा-ए-मुख़्तफ़ी को अलिफ़ से बदला, उर्दू वाले इस तरह के क़ाफ़िए को जाएज़ समझते हैं, वजह ये है की क़ाफ़िए में हुरूफ़-ए-मल्फ़ूज़ा का ए’तिबार है (या’नी spoken letters, not written letters) जब ये ‘हे’ मल्फ़ूज़ नहीं, (या’नी इस से ‘हे’ की आवाज़ नहीं आ रही) बल्कि (इसके पहले हर्फ़) ज़ के इशबाअ’ से अलिफ़ पैदा हो रहा है, तो फिर कौन माने’ है उसे हर्फ़-ए-रावी क़रार देने से? इसी तरह फ़ौरन (तन्वीन) और दुश्मन क़ाफ़िया हो जाता है, गो रस्म-उल-ख़त (script) उसके ख़िलाफ़ है।’’
शरह दीवान-ए-ग़ालिब अज़ तबातबाई
बात वाज़ेह है कि नज़्म तबातबाई ख़ुद भी हर्फ़ की आवाज़ और उसकी मल्फ़ूज़ी हैसियत को क़ाफ़िए के लिए शर्त मानते थे न कि तहरीरी हैसियत को, और ग़ालिब के अशआ’र से भी उन्हेोंने ग़ालिब का यही मौक़फ़ अख़्ज़ किया है।
नज़्म तबातबाई ज़बरदस्त शायर होने के साथ कई ज़बानों पर न सिर्फ़ उ’बूर रखते थे बल्कि अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी समेत कई ज़बानों की अदबी और शे’री रिवायत को भी ख़ूब जानते थे। मुकम्मल दीवान-ए-ग़ालिब के पहले शारेह थे, कई नज़्मों का तर्जुमा उर्दू में किया जिन में थोमस ग्रे की “ellegy written in a country churchyard” भी शामिल है जिसका मंज़ूम तर्जुमा उन्होंने ‘‘गोर-ए-गरेबाँ’’ के उन्वान से किया।
ग़ालिब की एक और ग़ज़ल जिसके क़वाफ़ी हैं ”जो, तो, हो,” वग़ैरा और रदीफ़ है ‘‘तो क्यूँकर हो’’ इसमें एक शे’र में ग़ालिब ने क़ाफ़ीया ‘वो’ लिया है, जब कि ‘वो’ का इमला ‘वाव’ और ‘हे’ है, और इस ग़ज़ल के बाक़ी तमाम क़वाफ़ी में हर्फ़-ए-रावी ‘वाव’ है (तो में ते और वाव, हो में हे और वाव) ग़ालिब ने ‘वो’ को इमला वाव और वाव लिखा है, (وو) वाव और हे नहीं।
शरह-ए-तबातबाई में इस शे’र के ज़ेल में लिखा हैः-
‘‘हमें फिर उनसे उमीद और उन्हें हमारी क़द्र
हमारा हाल ही पूछें न वो तो क्यूँकर हो
‘वो’ की ‘हे’ को क़ाफ़िए के लिए ‘वाव’ बना लिया है, इसलिए कि ये ‘हे’ तलफ़्फ़ुज़ में नहीं है, बल्कि
इज़हार-ए-हरकत-ए-मा-क़ब्ल के लिए है, (या’नी इस से पहले जो हर्फ़ है, उस पर जो भी हरकत है ज़बर, ज़ेर या वाव की, उसी हरकत को खींचने के लिए है, या’नी अगर ज़बर है तो ये ‘हे’ अलिफ़ की आवाज़ देगी, आगर ज़ेर है तो ‘ये’ की आवाज़ देगी आगर पेश है तो ‘वाव’ की आवाज़ देगी) जैसे लाला, ज़ाला, न, कि, (لالہ ژالہ نہ کہ) वग़ैरा में है, तो दूसरा वाव महज़ इश्बाअ’-ए-हरकत से पैदा हुआ है, और यही हर्फ़-ए-रावी है’’
(शरह दीवान-ए-ग़ालिब अज़ तबातबाई)
गोया कहना चाह रहे हैं कि ग़ालिब आगर ‘वाव’ न भी लिखते और सही इमला लिखते हुए ‘हे’ लिखते तब भी ये क़ाफ़िया दुरुस्त होता क्यूँकि ‘वाव’ की आवाज़ आ रही है, और हर्फ़-ए-रवी ‘वाव’ ही माना जाता क्यूँकि ए’तिबार हर्फ़-ए-मलफ़ूज़ा (spoken letters) का होता है और हुरूफ़-ए-मख़तूबा(written letters) का नहीं।
इमाम ख़लील फ़राहिदी, इल्म-ए-नहव के इमाम, इल्म-ए-अरूज़ के इमाम, अरबी अरूज़ के पहले मुरत्तिब थे, उन्हें बानी-ए-अरूज़ भी कहा जाता है, ये जो आज सब लोग ”फ़ाएलातुन फ़ाएलातुन” करते फिर रहे हैं ये सारा सिलसिला उन तक पहुंचता है, अरबी की पहली डिक्शनरी उन्होंने लिखी, उन्होंने जो क़ाफ़िए की ता’रीफ़ की है उसकी शुरूआ’त ऐसे की है ‘‘हिया मजमू-उल-असवात मिन आख़िरी बैत’’ मजमू-उल-हुरूफ़ नहीं कहा। बल्कि कहा के क़ाफ़िया कुछ आवाज़ों का मजमूआ’ है जो शे’र के आख़िर में होता है।
ग़ज़ल का हुस्न ही है कि एक आवाज़ के तकरार से एक हसीन आहंग पैदा हो न की ये कि लिखी हुई शक्ल देखने में अच्छी लगे। आगर बसरी क़ाफ़िए (या’नी दिखने में एक जैसे क़ाफ़िए) की इतनी अहमियत होती और ग़ज़ल का हुस्न सुनने से ज़ियादा लिखी हुई दिखने में होता तो शायर ज़बान सीखने से ज़ियादा ख़ुश-ख़ती (calligraphy) सीखते।
इन्हीं सब वजूह की बिना पर मेरा मानना है कि,
1– आगर कोई सौती क़ाफ़िए का क़ाएल नहीं तो न बाँधे। जो जाएज़ मानता है वो बाँधे।
2– इमला (spelling) में चाहे बदलाव न किया जाए, लेकिन आवाज़ पर क़ाफिये की बुनियाद हो।
3– कसक और सबक़ जैसे क़रीब-उल-मख़रज अल्फ़ाज़ को मैं हम-क़ाफ़िया नहीं मानता, वजह ये है कि उर्दू सौतियत में इनकी आवाज़ें अलग अलग हैं।
4– मात और साथ को ख़ूब बरता गया है इस लिए जाएज़ है लेकिन बचा जा सके तो बेहतर।
5– जिनकी आवाज़ में कोई फ़र्क़ नहीं, या’नी उर्दू में हम-मख़रज हैं, चाहे अरबी में मख़ारिज अलग हों जैसे ख़त और मत, राज़ और साज़, इन में कोई क़बाहत नहीं। यही तनवीन और नून का मुआ’मला है मेरे नज़दीक।
6– अलिफ़ और हा-ए-ग़ैर मलफ़ूज़ी पर ख़त्म होने वाले अल्फ़ाज़ को हम-क़ाफ़िया मानता हूँ चाहे मतले में ए’लान हो या न हो। मसलन दरिया और काबा।
आख़िरी बात ये है कि कुछ असातिज़ा ने इसे ना-जाएज़ माना है तो कुछ ने जाएज़ माना है। ऐसा नहीं है कि इत्तिफ़ाक़-ए-राय से इसे ऐ’ब माना गया हो। इस लिए जो जिसकी चाहे पैरवी करे कोई मसला नहीं है। आपको नहीं पसंद तो सौती क़ाफ़िया आप मत बाँधिए, आप को पसंद है तो बाँध लीजिए।
ये बिलकुल वैसा ही है जैसे कभी इख़्तिलाफ़ था, मसदर की सूरत का, कि ‘‘बात कहना है’’ दुरुस्त है या ‘‘बात कहनी है” दुरुस्त है, शुरू शुरू में बहुत शिद्दत से दोनों फ़रीक़ (both parties) अपने अपने मौक़फ़ पे अड़े रहे और फिर ‘‘ख़ैर-उल-उमूरी औसतुहा’’ (best path is the middle path) वाला मुआमला हो गया, या’नी वक़्त के साथ जो अवाम और लहजों का इख़्तिलात बढ़ा तो रफ़्ता रफ़्ता एक दरमियानी सूरत अपने आप वजूद में आती चली गई, शिद्दत ख़त्म हुई और दोनों फ़रीक़ की कुछ बातें क़ुबूल होती गईं और कुछ आवाम की ज़बान पर न चढ़ने की वजह से रद्द हो गईं।
ख़ैर ये अलग मसला है, बस ये बताना है कि क़वाइद जाने कितने थे, जो जब मौजूद ही नहीं हैं, ‘क़ाफ़िया-ए-मामूला’ ऐ’ब माना जाता था बाद में बाज़ ने उसे हुस्न माना कि ग़ज़ल में एक बार ऐसा क़ाफ़िया आना, हुस्न बढ़ाता है। बे-ख़ुद देहलवी लिखते है कि क़ाफ़िया-ए-मामूला जो दिल-कश और दिलचस्प हो, मुश्किल से हासिल होता है, इसी लिए शायर इस पर मरते हैं।
क़ाफिए की किताबों में क़ाफिया-ए-मामूला उसको कहते हैं जिस में क़ाफ़िया का कोई हिस्सा रदीफ़ में चला जाए। या रदीफ़ का कोई हिस्सा क़ाफ़िया में आ जाए। जैसे ग़ालिब की ग़ज़ल है जिसके क़वाफ़ी हैं, रवा, बोरिया, ग़ज़ल-सरा, और रदीफ़ है ‘‘न हुआ’’ इसी ग़ज़ल का एक मिस्रा है।
ले के दिल, दिल-सिताँ रवाना हुआ।
यहाँ रवाना एक लफ़्ज़ है जिसका एक हिस्सा क़ाफ़िए में आ गया और एक रदीफ में। इसे ऐब माना जाता था, और कहा जाता था कि इस से शे’र सुस्त हो जाता है, शायद ‘‘सुस्त’’ से मुराद ये है कि जब कोई ग़ज़ल पढ़ रहा हो तो रदीफ़ क़ाफिए उसके ज़ेहन में बैठ गए हैं अब अचानक उस क़ाफ़िए से इंहिराफ़ होगा तो फ़ौरन क़ारी या सामे’, का ज़ेहन सही लफ़्ज़ समझ नहीं पाएगा और शे’र समझने में वक़्त लगेगा।
लेकिन फिर समझ आने लगा कि यही मज़ा है इस क़ाफ़िए का, कि आगर इसे सलीक़े से बाँधा जाए तो जो हैरान करने वाली सलाहियत इसमें है वो शेर का हुस्न और दो-बाला करेगी।
ग़ालिब की एक ग़ज़ल का मतला है,
ग़म-ए-दुनिया से गर पाई भी फ़ुर्सत सर उठाने की
फ़लक़ को देखना तक़रीब तेरी याद आने की
क़ाफ़िए हैं उठाने आने और रदीफ़ है ”की”
इसी ग़ज़ल का शे’र है
कहूँ क्या ख़ूबी-ए-औज़ा-ए-अब्ना-ए-जमाँ ‘ग़ालिब’
बदी की उस ने जिस से हम ने की थी बार-हा नेकी
यहाँ काफ़िया-ए-मामूला इस्तिमाल किया है।
नज़्म तबातबाई इस शे’र की तशरीह में लिखते हैः-
‘‘इस ग़ज़ल के सब शे’रों में ‘‘ने’’ जुज़्व-ए-क़ाफ़िया था, और इस शे’र में जुज़्व-ए-रदीफ़ हो गया है, क़वाइद-ए-क़ाफ़िया में इस क़िस्म के क़ाफ़िए को मामूल कहते हैं, और इसे उयूब-ए-क़ाफ़िया में शुमार किया है, लेकिन शोअरा-ए-तसन्नो पसंद इसे एक सनअ’त समझते हैं चुनाँचे अहली शिराज़ी ने अपनी मसनवी शहर-ए-हलाल में हर हर शे’र में क़ाफ़िया-ए-मामूला का इल्तिज़ाम किया है, इसी तरह मीर अब्बास मग़फ़ूर ने अरबी की मसनवी मुरस्सा में क़ाफ़िया-ए-मामूला की क़ैद को लाज़िम कर लिया है’’
या’नी वक़्त के साथ ऐब को हुनर में बदलते हुए भी देखा है, सो ये कोई दलील कभी नहीं हो सकती की फ़लाँ चीज़ ऐब इस लिए है क्यूँकि कुतुब में दर्ज है। कुतुब में जो उसकी वजूह लिखी हैं, उन वजूह पर बहस करना, और अगर दलीलें उनके ख़िलाफ़ मिल जाएँ तो उन उसूलों को तर्क करना ही किसी भी ज़बान-ओ-अदब का एक हिस्सा रहा है। वरना क्यूँकर ऐब को हुनर में बदला गया।
कितने ही अल्फ़ाज़ का इमला बदला है, पहले उर्दू में पाओँ(پاؤن) को पाँव (پانو) लिखा जाता था अब पाओँ ही इस्टैंडर्ड है। और ये सब तब्दीलियाँ, ज़बान-ओ-अदब का एक फ़ितरी अमल है, जो वक़्त के साथ ब-तदरीज होता है, कोई रोक नहीं सकता, वर्ना आज जो आप उसके, उसने वग़ैरा लिख रहे हैं आप ”ऊसको, ऊसने” लिख रहे होते कि यही राइज था, और अब मतरूक हो गया, वजह क्या रही? कि ज़बान जो बोलती है उसका ए’तिबार होता है कलम जो लिखता है वो मतरूक (reject) हो जाता है, क़लम, स्क्रिप्ट, तहरीर, लफ़्ज़ की मकतूबी शक्ल ये सब ज़बान के मुहताज हैं। आप देखिएगा कि आने वाले वक़्त में (منع دفع) मना’ और दफ़ा’ को मना और दफ़ा लिखा जाएगा, वजह यही है कि शेर में तो आप इसे सह-हर्फ़ी बाँध रहे हैं और चूँकि ऐन का तलफ़्फ़ुज़ हमारे यहाँ नहीं है और उस पर भी ऐन-ए-साकिन, तो आप ख़ुद इसे सही नहीं बोल पाते, या’नी शे’र में वज़्न लेते हैं फ़े’ल (فعْل) का (21) और बोलते हैं फ़उ’ल (فعُل) के वज़्न पर (12)
बहुत से अहल-ए-फ़न ने यह रिआ’यत लेनी शुरू भी कर दी है।
तो बस किसी भी मौक़फ़ की बुनियाद तहक़ीक़ हो, दलाइल हों, और मा-कब्ल में की गई तहक़ीक़ का सही तजज़िया हो, सिर्फ़ इस वजह से किसी भी चीज़ को जाएज़ न माना जाए कि फ़लाँ ने किया है या कहा है तो ये जाएज़ फ़ुलाँ ने इसे मना’ किया है तो ना-जाएज़। ये एक मंतक़ी मुग़ालता या’नी logical fallacy है जिसे मुनाज़रे और मंतिक़ी बहस की इस्तिलाह में तवस्सुल बिल मरज’इया, या दलील-ए-एहतराम (appeal to authority) कहा जाता है।
ज़बान में सबसे बड़ी दलील रिवाज है, मैं हमेशा एक बात दोहराता हूँ कि डिक्शनेरी या किताबें ज़बान का रिवाज तय नहीं करतीं बल्कि रिवाज अस्ल है और डिक्शनेरी ताबे’ है, डिक्शनेरी हर कुछ रोज़ में ख़ुद को रिवाज-ए-आ’म के मुताबिक़ करती रहती है।
अख़िरी और सबसे अहम बात, कि बिना जाने रिआयत लेना कुछ मज़ेदार बात नहीं है, आप सीखें, पढ़ें, वजहें जानें, फिर किसी दलील की बिना पर रिआयत लें तो ये बेहतर तरीक़ा है। क्यूँकि तब आपका मक़सद हुस्न बढ़ाना होगा, न कि सिर्फ़ लिबर्टी लेना।
अपने इस शे’र पर बात ख़त्म करता हूँ,
सभी रस्में मोहब्बत की विसाल-ए-यार तक ही हैं
तेरी मर्ज़ी तू काबे में किसी रुख़ भी मुसल्ला रख
(विसाल-ए-यार से पहले ये लिबर्टीज़ नहीं मिलती)
NEWSLETTER
Enter your email address to follow this blog and receive notification of new posts.




