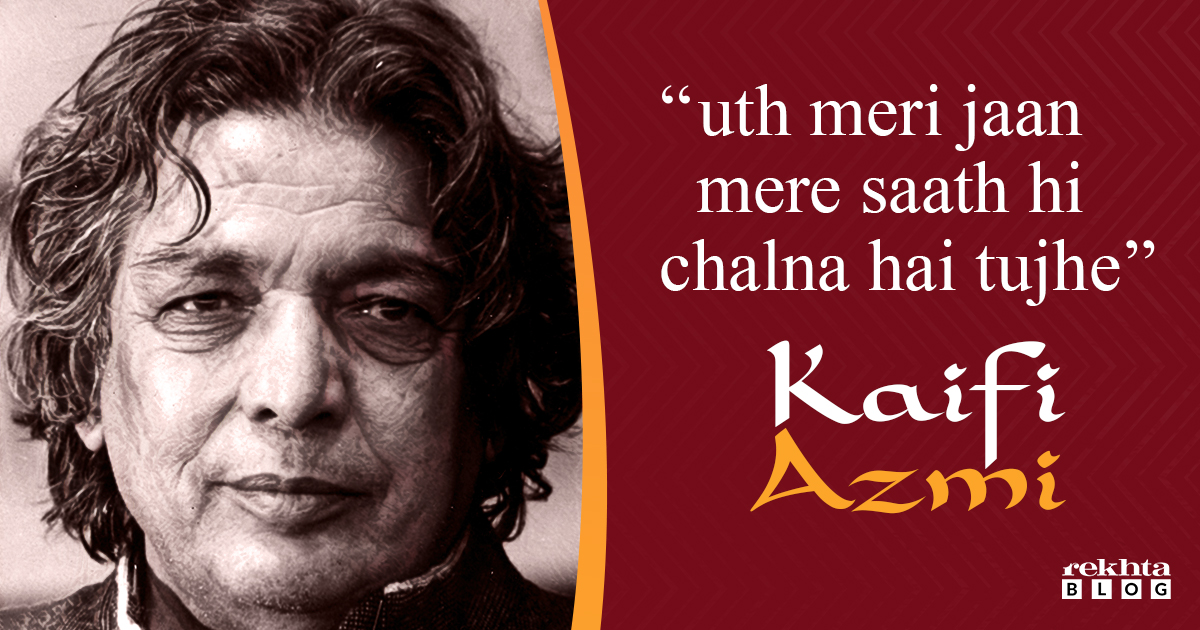
कैफ़ी आज़मी: एक सच्चे तरक़्क़ी-पसंद की ज़िंदगी और शायरी का क़िस्सा
कैफ़ी आज़मी अभी नौ-उम्र ही थे और शायर के तौर पर उनकी पहचान अभी उनके चंद दोस्तों तक ही सीमित थी कि वो बहराइच के एक मुशायरे में जा पहुँचे। मुशायरे की सदारत जिगर मुरादाबादी फ़रमा रहे थे। जिगर ने कुछ अपनी इश्क़िया ग़ज़ल-गोई और कुछ मय के ख़ुमार में जदीद नज़्म-निगारी और उसके एहतजाजी विषयों की आलोचना शुरू कर दी। जिगर की ये बातें कैफ़ी को बहुत नागवार गुज़रीं। कैफ़ी ने बरजस्ता जिगर की मुख़ालिफ़त में शेर कहे और बर-सर-ए-आम मुशायरे में पढ़ दिए। शेर ये थे,
तबीअत-ए -जब्र ये तसकीन से घबराई जाती है
हँसू कैसे हंसी कम्बख़्त तो मुरझाई जाती है
मेरे मुतरिब ना दे मुझको दावत-ए-नग़्मा
कहीं साज़-ए-गु़लामी पर ग़ज़ल भी गाई जाती है
जब जिगर ने ये शेर सुने तो जदीद नज़्मों पर दिए गई अपनी टिप्पणी पर शर्मिंदा हुए और कैफ़ी आज़मी से माफ़ी मांगी।
कैफ़ी शुरूआत से ही रौशन-ख़्याली, एहितजाजी तबीअत और शायरी के दक़्यानूसी विषयों से गहरी नाराज़गी के साथ आगे बढ़े थे। वो नहीं चाहते थे कि उर्दू शायरी या कोई भी फ़न सिर्फ़ सुरुर, दिल-लगी और वक़्त-गुज़ारी का ज़रीया बन कर रह जाये। वो शायरी को अपने उन ख़्यालात-ओ-जज़्बात के इज़हार के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे जो उनके दिल में दबे-कुचले, मज़्लूम, शोषण का शिकार, सामाजिक और आर्थिक सतह पर गु़लामी की ज़िंदगी बसर कर रहे लोगों को देखकर पैदा हुए थे।
मजवाँ से लखनऊ तक
कैफ़ी का जन्म आजमगढ़ के एक छोटे से गाँव मजवाँ में 1918 को हुआ था। उनका ख़ानदान पुराने ख़्यालात का जागीरदार ख़ानदान था। जहाँ न शिक्षा थी और न नए ख़्यालात की वो आज़ादी जिसे लेकर कैफ़ी जन्मे थे। भरे-पुरे ख़ानदान में सिर्फ़ कैफ़ी के पिता ही ऐसे थे जो किसी हद तक तालीम-याफ़्ता थे और चाहते थे कि उनके बच्चे भी गाँव की फ़िज़ा से बाहर निकल कर शिक्षा प्राप्त करें।
ख़ानदान की शदीद मुख़ालिफ़त के बावजूद कैफ़ी के पिता अपने बच्चों को लेकर लखनऊ आ गए और अवध की रियासत ‘तलहरा’ में तहसीलदार की नौकरी करने लगे। कैफ़ी आज़मी लिखते हैं, ”अब्बा के इस फ़ैसले से ख़ानदान में कोहराम मच गया कि ये कितना ग़लत क़दम है। अपना राज-पाट छोड़ कर नौकरी कर ली और सारे ज़मीन-दारों की नाक कट गई।”

कैफ़ी आठ भाई बहनों में सबसे छोटे थे। पिता ने कैफ़ी के तीन बड़े भाईयों को आधुनिक शिक्षा की तरफ़ लगा दिया था। कैफ़ी की चार बहनें बद-क़िस्मती से एक ख़तरनाक बीमारी का शिकार हो कर यके-बाद-दीगरे गुज़र गईं थीं। जिससे दुखी हो कर कैफ़ी के पिता ने सोचा कि ये मुसीबत हम पर इसलिए न आई है कि हमने सभी बच्चों को दुनियावी शिक्षा में डाल दिया है। सो उनके पिता ने फ़ैसला किया कि कैफ़ी को धार्मिक शिक्षा में लगाएँगे। ताकि मरते वक़्त कोई तो ऐसा हो जो हम पर फ़ातिहा पढ़ सके।
सुल्तान-उल-मदारिस और मज़हब पर फ़ातिहा
पिता के इस फ़ैसले के बाद बारह-तेरह बरस के कैफ़ी को लखनऊ की एक मशहूर धार्मिक दर्सगाह सुलतान-उल-मदारिस में दाख़िल करा दिया गया। कैफ़ी की मज़हबी तालीम जारी ही थी कि उन्हें मदरसे के क़ायदे-क़ानून, वहाँ की वय्वस्था, और मौलवियों की दुनिया से बेज़ारी पैदा हो गई। उन्होंने छात्रों की एक अन्जुमन बनाई और छात्रों की मांगों और उनकी जरूरतों का एक ख़ाका लेकर इंतेज़ामिया से भिड़ गए। मदरसे के मौलवियों के बनाए हुए उसूलों और ज़ाबतों के ख़िलाफ़ कैफ़ी और उनकी बनाई अंजुमन का एहतिजाज और स्ट्राइक का सिलसिला तक़रीबन एक साल तक जारी रहा।
इन दिनों कैफ़ी हर रोज़ इन्क़िलाबी नौईयत की एक नज़्म कहते और तलबा के जलूस में उसे पढ़ते ताकि विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे छात्रों के इरादों को मज़बूत किया जा सके। मदरसे के छात्र-विरोधी क़ानून के ख़िलाफ़ कैफ़ी की इस जद्द-ओ-जहद ने ही उनके दिल में दबी हुई इन्क़िलाब और एहतिजाज की चिंगारी को एक शक्ल दी और उनकी शायरी को एक मौक़ा दिया।
कैफ़ी लिखते हैं, ”मेरी शायरी की इब्तिदा एक रिवायती ग़ज़ल से हुई थी लेकिन इस स्ट्राइक के दौरान ग़ज़ल-गोई छूट गई और मैं एहितजाजी शायरी करने लगा। रोज़ एक नज़्म लिख कर लड़कों को सुनाता और उनमें जोश पैदा करता”
स्ट्राइक के नतीजे में कैफ़ी को मदरसे से निकाल दिया गया और उनके पिता का सपना की कैफ़ी मज़हबी आलिम बन कर उनकी आख़िरत में काम आएँ गए अधूरा रह गया। आयशा सिद्दीक़ी लिखती हैं, ”जो कैफ़ी मदरसे में इस लिए भेजे गए थे कि फ़ातिहा पढ़ना सीख जाएँ वो ख़ुद मज़हब पर फ़ातिहा पढ़ कर वहाँ से निकल आए।”
मुंबई का सफ़र और तहरीक से वाबस्तगी
लखनऊ के मदरसे के निज़ाम के ख़िलाफ़ कैफ़ी की स्ट्राइक और उनकी इन्क़िलाबी नज़मों का असर ये हुआ कि वो लखनऊ में मौजूद तरक़्क़ी-पसंद लोगों की नज़र में आ गए। अली अब्बास हुसैनी, एहतिशाम हुसैन, अली सरदार जाफ़री और सज्जाद ज़हीर से उनकी मुलाक़ातें होने लगीं। कैफ़ी की सलाहियतों, उनके इन्क़िलाबी जोश-ओ-जज़्बे को देखकर सरदार जाफ़री और सज्जाद ज़हीर उन्हें मुंबई ले आए। 1943 में कैफ़ी ने मुंबई की राह ली और यहाँ एक शायर-ओ-सहाफ़ी की हैसियत से चालीस रुपय महीना की तनख़्वाह पर काम करने लगे।
इन दिनों मुंबई सियासी और इन्क़िलाबी तहरीक का मरकज़ बना हुआ था। कैफ़ी के लिए ये सारा माहौल बहुत साज़गार साबित हुआ। उन्हें वो मैदान मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। राज बहादुर गौड़ लिखते हैं, ”मुंबई आने के बाद कैफ़ी मज़दूरों में रहने लगे उन्हें शेर सुनाते, उनके दुख-दर्द को सुनते, ‘क़ौमी जंग’ में लिखते और ‘क़ौमी जंग’ को सड़कों पर बेचते फिरते।”

मुंबई आने के कुछ महीने बाद ही कैफ़ी का पहला काव्य संग्रह ‘झनकार’ प्रकाशित हुआ। जिस पर तरक़्क़ी-पसंदों के सालार सज्जाद ज़हीर ने अपनी राय देते हुए लिखा था,
”जदीद उर्दू शायरी के बाग़ में एक नया फूल खिला है, एक सुर्ख़ फूल”
ये सुर्ख़ फूल वक़्त के साथ-साथ और सुर्ख़ होता गया।
मुंबई की कम्यूनिस्ट पार्टी से जुड़ने के बाद कैफ़ी को ‘नागपाड़ा’ इलाक़े की रीज्नल कमेटी का सिक्रेटरी बना दिया गया था। कैफ़ी ने वहाँ रह कर मज़दूरों को इखट्टा करने की कोशिश की और उन्हें उनके हुक़ूक़ के लिए जागरुक किया।
ये सारे संघर्ष और ये सारी जिद्द-ओ-जहद कैफ़ी आज़मी की शयारी के लिए ग़िज़ा फ़राहम कर रही थी। कैफ़ी की शायरी उस तरक़्क़ी-पसंद की शायरी नहीं थी जो ड्राइंग-रूम में आराम से बैठ कर मिस्रे जोड़ रहा हो। कैफ़ी तो इस जद्द-ओ-जहद और संघर्श का हिस्सा थे जो सड़कों, गलियों और मौहल्लों में किया जा रहा था। कैफ़ी मुंबई के गली-कूचों में जाते, तक़रीरें करते, अपनी नज़्में सुनाते और कभी-कभी मार भी खाते। उनकी मशहूर नज़्म ‘मकान’ इसी दौर की यादगार है जब वो ‘मदनपूरा’ के फुट-पाथ पर बैठे अपने दुख-दर्द को मिस्रों में ढाल रहे थे।
आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है
आज की रात न फ़ुट-पाथ पे नींद आएगी
सब उठो, मैं भी उठूँ तुम भी उठो, तुम भी उठो
कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी
नज़्म ‘औरत’ की मक़बूलियत
उन्हीं दिनों कैफ़ी ने अपनी मशहूर नज़्म ‘औरत’ लिखी। इस नज़्म की मक़बूलियत का ये आलम था कि कैफ़ी जहाँ जाते, जिस मजलिस में होते उनसे ये नज़्म सुनी जाती। कैफ़ी अभी नौजवानी ही थे लेकिन औरत और उसके वुजूद को देखने का उनका नज़रिया बिलकुल मुख़्तलिफ़ था। वो जिन शदीद लफ़्ज़ों में औरत की आज़ादी और ख़ुद-मुख़्तारी का तराना गए रहे थे उसने उन्हें अपने वक़्त के शायरों में बहुत मुम्ताज़ बनाया दिया था।
उठ मिरी जान मिरे साथ ही चलना है तुझे
क़ल्ब-ए-माहौल में लर्ज़ां शरर-ए-जंग हैं आज
हौसले वक़्त के और ज़ीस्त के यक-रंग हैं आज
आबगीनों में तपाँ वलवला-ए-संग हैं आज
हुस्न और इश्क़ हम-आवाज़ ओ हम-आहंग हैं आज
जिस में जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे
उठ मिरी जान मिरे साथ ही चलना है तुझे
कैफ़ी की पत्नी शौकत कैफ़ी एक शेरी मजलिस का ज़िक्र करते हुए लिखती हैं, ”जब एक छोटी सी निजी महफ़िल में वाई बी चौहान ने ये नज़्म सुनी तो बोले, ”कैफ़ी को सदियों तक ज़िंदा रखने के लिए ये एक नज़्म ही काफ़ी है।”
शौकत कैफ़ी से मुलाक़ात, मुहब्बत और शादी
यही वो नज़्म थी जिसने शौकत को भी बहुत प्रभावित किया था और कैफ़ी आज़मी में उनकी दिलचस्पी को बढ़ावा दिया था। शौकत और कैफ़ी की मुलाक़ात हैदराबाद में हुई थी। यहाँ कैफ़ी 1947 में एक मुशायरे के लिए पहुँचे थे। उस ज़माने में उनकी मक़बूलियत का एक दूसरा ही आलम था। शौकत जो उस वक़्त तक शौकत कैफ़ी नहीं बनी थीं, बताती हैं, ”हैदराबाद के वीमेंस कॉलेज में कैफ़ी की तस्वीरें 25 और 30 रूपयों में बिका करती थीं। कैफ़ी लड़कियों के बहुत महबूब शायर थे।”

हैदराबाद में कैफ़ी अपने तरक़्क़ी-पसंद दोस्तों सरदार जाफ़री और मजरूह सुलतानपुरी के साथ मुशायरा पढ़ने पहुँचे थे। सुनने वालों में शौकत भी मौजूद थीं। आगे का क़िस्सा शौकत कैफ़ी ख़ुद सुनाती हैं,
“मैं दुबली-पतली सी लड़की सेहर-ज़दा बैठी थी, इस नौजवान की गरजदार आवाज़ सुनकर सेहर-ज़दा हो रही थी। मुशायरा ख़त्म हुआ, कैफ़ी को लड़कियों ने घेर लिया, ऑटोग्राफ के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है कैफ़ी की उस वक़्त की पोज़ीशन किसी हीरो से कम नहीं थी। जब ये दुबली-पतली लड़की अपनी ऑटोग्राफ बुक लेकर उनके पास पहुँची तो कैफ़ी ने शरारत से एक बे-अर्थ शेर उस पर लिख दिया। उस लड़की की खुद्दारी को बहुत ठेस लगी। जब घर पहुँची तो सीढ़ीयाँ चढ़ते हुए इस लड़की ने शिकायत की, “आपने हमारी ऑटोग्राफ़ बुक पर इतना बुरा शेर क्यों लिखा? कैफ़ी मुस्कुराए और इसी लहजे में बोले, आपने सबसे पहले हम से ऑटोग्राफ़ क्यों नहीं लिया? दोनों खिलखिला कर हँस पड़े और आँखों ने आँखों से कुछ कहा, कैफ़ी की नज़्म के इन मिस्रों की तरह,
दो निगाहों का अचानक वो तसादुम मत पूछ
ठेस लगते ही उड़ा इश्क़ शरारा बन कर
शौकत आगे बताती हैं कि, उन आँखों के तसादुम ने घर वालों में एक हंगामा-ख़ेज़ तसादुम बरपा कर दिया था। लेकिन तमाम मुख़ालिफ़तों के बावजूद कैफ़ी और शौकत की शादी हो गई।
हुकूमत की ज़्यादतियाँ, रूपोशी और कैफ़ी की मुश्किलें
शादी के बाद शौकत और कैफ़ी मुंबई आ गए। अब कैफ़ी अकेले नहीं थे उनके साथ शौकत भी थीं, उनके कामों में सहारा देतीं हुईं। कैफ़ी के काम ही क्या थे, मज़दूरों के बीच रहना, उन पर हो रहे ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना और पार्टी के नज़रियात को आम करने में जी-जान से मेहनत करना। शौकत कैफ़ी बताती हैं, ”हम कई-कई मील दूर पैदल चल कर जुलूस निकालते, इन्क़िलाब ज़िंदाबाद, कम्यूनिस्ट पार्टी ज़िंदाबाद, किसान मज़दूर की जय हो का नारा लगाते।”
एक वक़्त वो आया जब पार्टी हुकूमत की ज़्यादतियों का शिकार हुई और उसके लीडरों को जेलों में डाला जाने लगा तो कैफ़ी रुपोश हो गए। अंडर-ग्राउंड रह रहे कैफ़ी से शौकत की मुलाक़ातें महीनों में होतीं। शौकत कैफ़ी लिखती हैं, ”एक बार महीनों बाद उनसे अँधेरी के एक घर में मुलाक़ात हुई तो उन्हें पहचाना ही नहीं। उन्होंने मूँछें रख ली थीं, मैंने कहा, तौबा क्या शक्ल बना ली है, बिल्कुल पुलिस कांस्टेबल लगते हो। कैफ़ी हंसकर बोले, इसी लिए तो जेल जाने से बचा हुआ हूँ।”
ये दिन कैफ़ी और शौकत के लिए आर्थिक तौर पर बहुत सख़्त थे। पार्टी कामों में लगे रहने से कुछ पैसे मिलते थे लेकिन वो इतने कम थे कि दोनों की मुश्किल से गुज़र-बसर होती थी। इसी दौरान शौकत और कैफ़ी के एक बच्चा पैदा हुआ जो चंद महीनों के बाद ही ग़ुर्बत की वजह से एक बीमारी का शिकार हो कर मर गया। बच्चे की मौत ने शौकत और कैफ़ी को हिला कर रख दिया।
इसके बाद शौकत ने एक बेटी को जन्म दिया। जिसका नाम शबाना रखा गया। हमारे आज के समय की प्रसिद्ध अदकारा शबाना आज़मी। शबाना की पैदाइश के बाद कैफ़ी ने इरादा कर लिया था कि अपने दूसरे बच्चे को ग़ुर्बत और पैसे की कमी होने की वजह से नहीँ मरने दूँगा। शौकत कैफ़ी लिखती हैं, ”कैफ़ी को ये फ़िक्र थी पहला बच्चा तो ग़ुर्बत की नज़र हो गया। अब इस बच्ची के लिए उन्हें पैसा कमाना चाहिए।”
फिल्मों से वाबस्तगी
शबाना की परवरिश और घर की जरूरतों को पूरा करने की ज़िम्मेदारी का यही एहसास था कि कैफ़ी गाने लिखने के लिए फ़िल्मी दुनिया की तरफ़ चले गए। वर्ना उनके लिए पार्टी, पार्टी के नज़रियात और उनकी तशहीर और ग़रीब अवाम के बीच होना सबसे बुनियादी काम था। वो फिल्मों में लिखने के साथ अपने इन कामों को भी वैसे ही करते रहे।
कैफ़ी ने फिल्मों के लिए गाने के इलावा मुकालमे, मंज़रनामे और कहानियाँ भी लिखीं। जिसके लिए उन्हें फ़िल्म फ़ेयर के कई अवार्ड से भी नवाज़ा गया। काग़ज़ के फूल, हक़ीक़त, हीर राँझा, गर्म हवा वग़ैरा उनकी अहम फिल्में हैं।
शबाना के लिए तोहफ़ा
शौकत कैफ़ी आर्थिक बदहाली के इन्हीं दिनों का एक और क़िस्सा सुनाती हैं। बताती हैं, “शबाना छोटी थी और उसे आम बहुत पसंद थे। घर में ज़्यादा पैसे होते नहीं थे इसलिए आम कम ही ख़रीदे जाते थे। एक बार शबाना अपनी दोस्त पर्ना के घर से दो दर्जन आम ले आई और ख़ुश हो कर मुझे बताने लगी, “मम्मी पर्ना के गाँव से आम आए थे तो उन्होंने इतने सारे आम मुझे भी दे दिए” शौकत आगे लिखती हैं, ”कैफ़ी के दिल में ये बात तीर की तरह चुभ गई। बोले कुछ नहीं।

बीमारी के बाद जब उन्हें अपने गाँव में रहने का ख़्याल आया तो पहला काम कैफ़ी ने ये किया कि मलीहाबाद से आम के सैकड़ों पेड़ गाँव ले गए और जब पाँच साल बाद बाग़ में आम आए तो सबसे पहले कई सौ आम शबाना के लिए ले कर मुम्बई आ गए।”
1973 के बाद के कैफ़ी
1973 को कैफ़ी फ़ालिज का शिकार हुए। ये वक़्त ना सिर्फ़ कैफ़ी बल्कि उनके घर के लोगों और उनके चाहने वालों, सभी के लिए मुश्किल का वक़्त था। लेकिन लंबे ईलाज के बाद वो सेहतयाब हो गए।
कैफ़ी अब मुंबई की ज़िंदगी से उकता गए थे। न अब मुंबई वो मुंबई रह गया था जो उस वक़्त था जब कैफ़ी वहाँ पहुँचे थे। उनके सारे तरक़्क़ी-पसंद दोस्त बिखर गए थे। तहरीक के कामों में भी वो शिद्दत न रही थी जिसके कैफ़ी आदी थे। कैफ़ी ने ज़िंदगी के बाक़ी बरस अपने गाँव ‘मजवां’ में गुज़ारने का फ़ैसला किया। कैफ़ी जब ‘मजवां’ पहुँचे तो उन्हें इस इलाक़े की बदहाली को देख बहुत दुख हुआ। कैफ़ी की इन्क़िलाबी तबियत ने फिर सँभाल लिया और वो इस इलाक़े की तरक़्क़ी और फ़लाह-ओ-बहबूद में लग गए। बहुत कम समय में कैफ़ी ने ‘मजवां’ की तस्वीर बदल कर रख दी। कैफ़ी को गाँव में रहना अच्छा लगता था। वो कहते थे, ”मैं किसान हूँ, मुझे ज़मीन से प्यार है और मुझे ज़मीन पर रहना अच्छा लगता है।”
सच्चा तरक़्क़ी-पसंद
कैफ़ी की ज़िंदगी, उनकी फ़िक्र और उनके कामों को देखा जाए तो समझ में आता है वो एक सच्चे तरक़्क़ी-पसंद के तौर पर अपना जीवन जी रहे थे। उन्होंने मज़दूरों, ग़रीबों और मज़लूमों की हिमायत में सिर्फ़ शायरी ही नहीं बल्कि सड़कों पर आ कर उनके लिए आवाज़ उठाई, नारे लगाए, लाठीयाँ खाईं और अपना जीवन हर तरह से उनके क़रीब रह कर गुज़ारा। ज़िंदगी की इस सरगर्मी से हासिल होने वाले तजुर्बे को शायरी का रूप दिया। सज्जाद ज़हीर कैफ़ी की शायरी के बारे में लिखते हैं,
”कैफ़ी की शायरी क़दीम-ओ-जदीद क़िस्म की अदबी ग़लाज़तों से पाक है। इस में सच्ची तरक़्क़ी-पसंदी की झलक नज़र आती है।”
यही सच्ची तरक़्क़ी-पसंदी की झलक है जो आज भी कैफ़ी की शायरी को ज़िंदा और बा-मानी बनाए हुए है।
NEWSLETTER
Enter your email address to follow this blog and receive notification of new posts.




