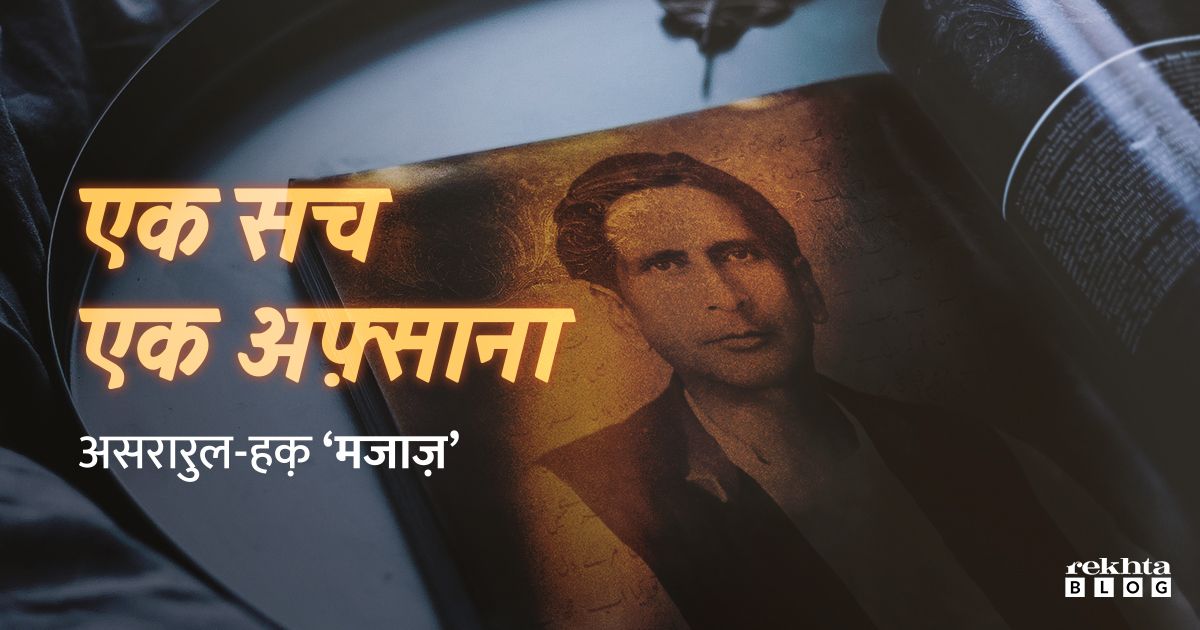
एक सच, एक अफ़साना : असरारुल-हक़ ‘मजाज़’
“वो बड़ा मुख़लिस, बड़ा दिल-नवाज़, बड़ा प्यारा इंसान था। वो सब का दोस्त था, सिर्फ़ अपना दुश्मन था। उस ने अपनी शाइ’री, अपनी सेह्हत, अपनी ज़िंदगी, सब अपनी कमज़ोरी की नज़्र कर दी। हम सब देखते रहे और कुछ न कर सके। उस की शाइ’री ख़ूबसूरत, पुर-सोज़, जवान और जानदार है, जो ज़िंदा रहेगी। उसे तो वक़्त का ज़ालिम हाथ भी नहीं मिटा सकता। उस की ज़हानत, उस की मोहब्बत, उस की दिल-रुबा शख़्सियत और उस की ज़िंदा-दिली की याद उसके दोस्तों के दिल से कभी मह्व न होगी।”
ये जुम्ले प्रोफ़ैसर आल-ए-अहमद ‘सुरूर’ ने ‘मजाज़’ के बारे उन के वालिद जनाब सिराजुल-हक़ को मजाज़ के इंतक़ाल के तीन दिन बा’द ता’ज़ियाती ख़त में लिखे थे। मगर क्या मजाज़ का तआ’रुफ़ और उस की मीरास बस यही है?
मजाज़ या’नी वो असरार जिन्हें दुनिया आज उस की मौत के 67 साल बा’द भी समझने की कोशिश में मुब्तला है। जिस के इ’श्क़, जुनून, मुहब्बत, हाज़िर-जवाबी, मयनोशी, और मौत के इर्द-गिर्द इतने क़िस्से सुने-सुनाए गए हैं कि उन में कौन सा सच और कौन सा अफ़्वाह है, फ़र्क़ करना मुश्किल है। वो शाइ’र जिस की शाइ’री लोगों की ज़िन्दगी बन गई, और जिस की ज़िन्दगी ख़ुद एक ग़मनाक शे’र। जो कहता था,
ख़ूब पहचान लो असरार हूँ मैं
जिंस-ए-उल्फ़त का तलब-गार हूँ मैं
इ’श्क़ ही इ’श्क़ है दुनिया मेरी
फ़ित्ना-ए-अ’क़्ल से बे-ज़ार हूँ मैं
ये दुनिया अफ़्साने पसंद करती है, इसे हज़ार रातों का अफ़्साना चाहिए, ये कभी अफ़्सानों से ऊबती नहीं, शायद इसी लिए इस ने मजाज़ की हक़ीक़त में भी अफ़्साने ही ढूँढे। मगर मजाज़ को उस के अधूरे इ’श्क़ और मयनोशी के अफ़्सानों से अलग उस के इंक़लाबी तेवर के साथ भी देखा जाना चाहिए।
मजाज़ की ज़िन्दगी हर तौर ख़ुद में एक इंक़लाब थी। उस ने केवल इंक़लाब लिखा नहीं, बल्कि जिया भी। चाहे वो वालिद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इंजीनियरिंग न करने का फ़ैसला हो, या सरकारी नौकरी में रह कर सरकार के ख़िलाफ़ नज़्में लिखना हो या फिर समाजी हदों के पार मुहब्बत करने की जुर्अत। ये सब मजाज़ के इंक़लाबी ज़ेहन के एक्सटेंशन ही थे। और शायद इन्हीं में उसने ख़ुद को डुबा दिया।
कमाल-ए-इ’श्क़ है दीवाना हो गया हूँ मैं
ये किस के हाथ से दामन छुड़ा रहा हूँ मैं
तुम्हीं तो हो जिसे कहती है ना-ख़ुदा दुनिया
बचा सको तो बचा लो कि डूबता हूँ मैं
मजाज़ के मज्मूआ’-ए-कलाम के दीबाचे में फैज़ अहमद ‘फैज़’ लिखते हैं, “मजाज़ की इंक़लाबियत आ’म इंक़लाबी शाइ’रों से अलग है। वो इंक़लाब को लेकर सीना कूटते हैं, गरजते हैं। मजाज़ इंक़लाब का मुतरिब है।”
मजाज़ इंक़लाब को नग़्मों में ढाल देता है और गाता है।
नहीं ये फ़िक्र कोई रहबर-ए-कामिल नहीं मिलता
कोई दुनिया में मानूस-ए-मिज़ाज-ए-दिल नहीं मिलता
कभी साहिल पे रह कर शौक़ तूफ़ानों से टकराएँ
कभी तूफ़ाँ में रह कर फ़िक्र है साहिल नहीं मिलता
शिकस्ता-पा को मुज़्दा ख़स्तगान-ए-राह को मुज़्दा
कि रहबर को सुराग़-ए-जादा-ए-मंज़िल नहीं मिलता
वहाँ कितनों को तख़्त-ओ-ताज का अरमाँ है क्या कहिए
जहाँ साइल को अक्सर कासा-ए-साइल नहीं मिलता
ये क़त्ल-ए-आ’म और बे-इज़्न क़त्ल-ए-आ’म क्या कहिए
ये बिस्मिल कैसे बिस्मिल हैं जिन्हें क़ातिल नहीं मिलता
मजाज़ कहीं किनारे खड़े होकर ना’रे नहीं लगाता, वो किसी आ’म नौजवान की तरह आज के हालात पर रोता भी है, उसे बदलने के लिए मुट्ठियाँ भी भींचता है, और बेहतर कल के हसीन ख़्वाब भी देखता है।
आवारा-ओ-मजनूँ ही पे मौक़ूफ़ नहीं कुछ
मिलने हैं अभी मुझ को ख़िताब और ज़ियादा
टपकेगा लहू और मिरे दीदा-ए-तर से
धड़केगा दिल-ए-ख़ाना-ख़राब और ज़ियादा
चूँकि मजाज़, ब-क़ौल फैज़ अहमद ‘फैज़’, “इंक़लाब के ढिंढोरची” नहीं है, बाज़ दफ़्अ’ उस के अशआ’र तरक्क़ी-पसंद और इंक़लाबी होते हुए भी इश्क़िया लगते हैं। और शायद यही मजाज़ की शायरी का ख़ासा है।
ये बिजली चमकती है क्यूँ दम-ब-दम
चमन में कोई आशियाना भी है
ख़िरद की इताअ’त ज़रूरी सही
यही तो जुनूँ का ज़माना भी है
मुझे आज साहिल पे रोने भी दो
कि तूफ़ान में मुस्कुराना भी है
ज़माने से आगे तो बढ़िए ‘मजाज़’
ज़माने को आगे बढ़ाना भी है
आज से कई दहाई पहले जब फ़ेमिनिज़्म लफ़्ज़ इतना आ’म नहीं था तब मजाज़ ने वो नज़्म कही जो आज भी हुक़ूक़-ए-निस्वाँ और आज़ादी का ज़िक्र होने पर दिल बे-साख़्ता गा उठता है :
हिजाब-ए-फ़ित्ना-परवर अब उठा लेती तो अच्छा था
ख़ुद अपने हुस्न को पर्दा बना लेती तो अच्छा था
तिरी नीची नज़र ख़ुद तेरी इ’स्मत की मुहाफ़िज़ है
तू इस नश्तर की तेज़ी आज़मा लेती तो अच्छा था
तिरे माथे पे ये आँचल बहुत ही ख़ूब है लेकिन
तू इस आँचल से इक परचम बना लेती तो अच्छा था
और अगर बात सर्वहारा वर्ग की हो तो मजाज़ की नज़्म “मज़दूरों का गीत” याद आती है :
मेहनत से ये माना चूर हैं हम
आराम से कोसों दूर हैं हम
पर लड़ने पर मजबूर हैं हम
मज़दूर हैं हम मज़दूर हैं हम
जिस सम्त बढ़ा देते हैं क़दम
झुक जाते हैं शाहों के परचम
सावंत हैं हम बलवंत हैं हम
मज़दूर हैं हम मज़दूर हैं हम
जिस रोज़ बग़ावत कर देंगे
दुनिया में क़यामत कर देंगे
ख़्वाबों को हक़ीक़त कर देंगे
मज़दूर हैं हम मज़दूर हैं हम
और अंत में वो नज़्म जिसका ज़िक्र किये बिन मजाज़ ही नहीं पूरे तरक्क़ी-पसंद उर्दू अदब की बात पूरी नहीं हो सकती। “आवारा” नज़्म ने मजाज़ को एक नई पहचान दी। उस दौर के हर नौजवान की बेचैनी और जद्द-ओ-जेहद को जैसे आवाज़ मिल गयी थी। “आवारा” का एहतिजाज, उस की बग़ावत, कोरा भाषण या ना’रा नहीं है, उस में रूमानियत है। रूमानियत जो वक़्त से परे हैं। और शायद इसी लिए ये नज़्म आज भी अदब का ज़ौक़ रखने वाले नौजवानों को पसंद आती है। ब-क़ौल अली सरदार जाफ़री, “यह नज़्म नौजवानों का ऐ’लान-नामा थी और आवारा का किरदार उर्दू शाइ’री में बग़ावत और आज़ादी का पैकर बनकर उभर आया है।”
शहर की रात और मैं नाशाद-ओ-नाकारा फिरूँ
जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूँ
ग़ैर की बस्ती है कब तक दर-ब-दर मारा फिरूँ
ऐ ग़म-ए-दिल क्या करूँ? ऐ वहशत-ए-दिल क्या करूँ?
मजाज़ की शख़्शियत और शाइ’री को लोगों ने अपने अपने तरीक़े से देखा, और सभी को अपने मतलब का कुछ उसमें मिल ही गया। किसी को रात भर जागने वाला जग्गन मिला, तो किसी को अधूरे इ’श्क़ के ग़म में डूबा आ’शिक़, किसी ने उस में उर्दू अदब का कीट्स देखा, तो किसी ने इंक़लाब का मुतरिब, किसी को ख़ुश-मिज़ाज, ख़ुश-लिबास मजाज़ मिला जिस पर यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ फ़िदा थीं, तो किसी को शराब के नशे में डूबा मजाज़ मिला जो तन्हाई का मारा था, किसी को उसकी हाज़िर-जवाबी के लतीफ़े मिले तो किसी को उस की दीवानगी के हौलनाक क़िस्से। मगर सचमुच मजाज़ कौन था, ये असरार शायद हमेशा बना ही रहेगा।
NEWSLETTER
Enter your email address to follow this blog and receive notification of new posts.




