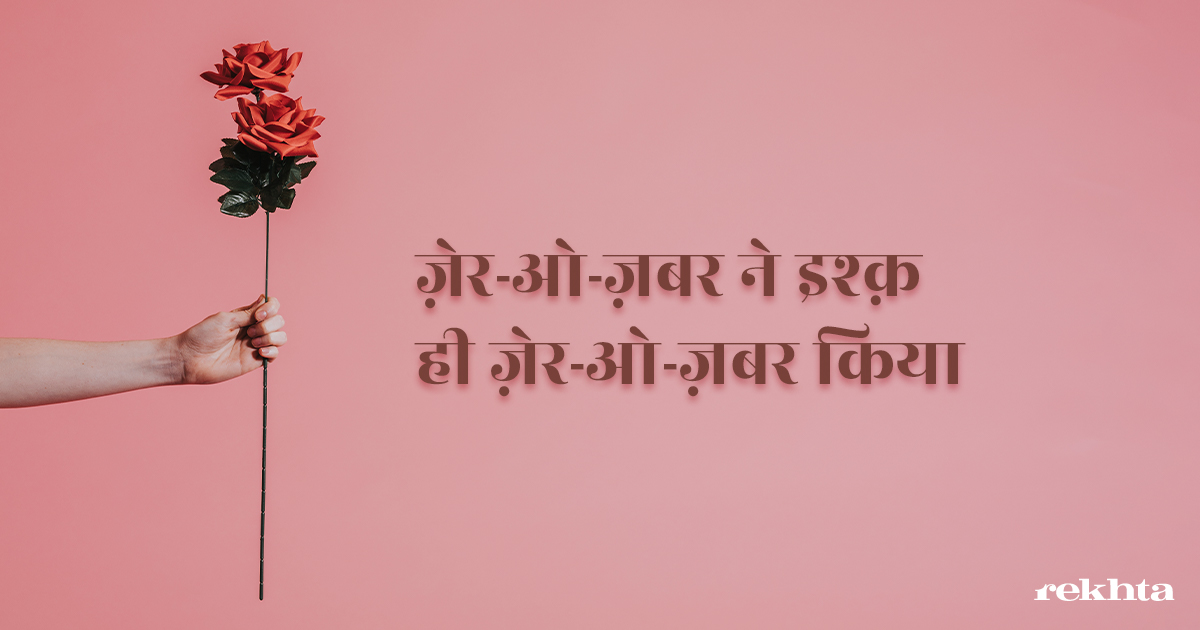
ज़ेर-ओ-ज़बर ने इश्क़ ही ज़ेर-ओ-ज़बर किया
मैंने जौन एलिया का एक शेर पढ़ा जो रोमन में लिखा हुआ और देवनागरी में भी,
जब वो निगार-ए-सह्सराम हमसे हुआ था हम-कनार
कौन ‘बहार’ का न था, कौन ‘बहार’ का नहीं
लिखने वाले ने लाशऊरी तौर पर मान लिया होगा कि शायरी के साथ ज़ियादा मुनासिब लफ़्ज़ “बहार” ही है, जबकि इसी शेर में पहले मिसरे में जो ‘सह्सराम’ है वो अस्ल में बिहार का एक इलाक़ा सासाराम है, जहाँ से ज़ाहिदा हिना साहिबा का तअल्लुक़ है।
तो दूसरा मिसरा अस्ल में यूँ हुआ,
“कौन बिहार का न था, कौन बिहार का नहीं”
किसी के लाशऊर (अवचेतन) को यह कितना भी ग़ैर-रूमानी मिसरा लगे, मुझे लुत्फ़ इसी में आ रहा है।
उर्दू सीखने/ पढ़ने वालों के लिये कभी कभी बड़ा मसअला हो जाता है उर्दू में ऐराब का ज़ाहिर न होना। यानी जैसे हिन्दी में छोटी ‘इ’ की मात्रा या छोटे ‘उ’ की मात्रा होती है, उर्दू में उसके लिये ”ज़बर, ज़ेर, पेश” होते हैं, लेकिन वो लिखते वक़्त ज़ाहिर नहीं किये जाते। अब “मुकम्मल” लिखा हो तो यह मुकम्मिल भी हो सकता है, मुकम्मुल भी पढ़ा जा सकता है, मिकम्मुल भी पढ़ा जा सकता है।
ज़बर ज़ेर के फ़र्क़ से कई मरतबा अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ‘मुकम्मल’ और ‘मुकम्मिल’ दो अलग लफ़्ज़ हैं और अलग अर्थ लिये हुये हैं। लेकिन लोग मुकम्मिल को भी मुकम्मल के मानी में ले लेते हैं। वहाँ तक तो मामला फिर भी चल जाता है, जहाँ अर्थ न बदल रहे हों, मसलन काफ़िर को काफ़र कह दिया, मगर जहाँ अर्थ/ मानी बदल जायें वहाँ यह ग़लती बहुत बड़ी हो जाती है।
आप सुनते होंगे कि अदालत में मुलज़िम की पेशी हुई, और मुलज़िम का अर्थ यह समझा जाता है कि वो शख़्स जिस पर किसी जुर्म का इलज़ाम हो। यह ग़लत इसतेमाल है, ‘मुलज़म’ सही लफ़्ज़ है इस जगह, मुलज़िम वो होता है जो इलज़ाम लगाये, जैसे मुजरिम वो जो जुर्म करे, मुनसिफ़ वो जो इंसाफ़ करे इसी तरह मुलज़िम वो जो इलज़ाम लगाये।
मुशायरों के स्टेज पर भी कभी सुनते हैं कि “फ़लाँ साहब को हमने सद्र मुनतख़िब किया है” यहाँ ‘मुनतख़ब’ होना चाहिये, ‘मुनतख़िब’ वो है जो किसी को सद्र बना रहा है, या selection/ इनतिख़ाब कर रहा है।
इसी तरह इक़बाल का मशहूर शेर है,
कभी ऐ हक़ीक़त-ए-मुन्तज़िर, नज़र आ लिबास-ए-मजाज़ में
कि हज़ार सजदे तड़प रहे हैं मिरी जबीन-ए-नियाज़ में
बहुत लोग इसमें “हक़ीकत-ए-मुन्तज़िर” पढ़ते हैं, हालाँकि सही लफ़्ज़ यहाँ ‘मुनतज़र’ है, और फ़र्क़ यह है कि ‘मुनतज़िर’ कहते हैं इंतज़ार करने वाले को, जैसे मुन्तज़िम इनतज़ाम करने वाले को, और ‘मुंतज़र’ उस को कहते हैं ‘जिसका इंतज़ार किया जाये’। अगर हम इस शेर में ‘मुन्तज़िर’ मानें तो शेर का मफ़हूम ही कुछ न रहेगा। शेर का मफ़हूम कुछ यूँ है “ऐ हक़ीक़त, मेरी जबीन के सजदे तड़प रहे हैं, कि तू सामने आये और वो तेरे सामने अदा हो जायें, तू अगर तूहक़ीक़ी हालत में सामने नहीं आ सकती तो मजाज़ी सूरत में ही दिख जा।” यानी मैं और मेरे सजदे इंतज़ार कर रहे हैं, तो यही मुन्तज़िर हैं, और वो हक़ीक़त जिसका इंतज़ार किया जा रहा है वो ‘मुनतज़र’ है। अगर हम उसे ‘मुनतज़िर’ पढ़ेंगे तो यह क्या बात हुई कि उसी का हम इंतज़ार कर रहे हैं और उसे ही इंतज़ार करने वाली मान रहे हैं।
इसी तरह जिगर का शेर जो बहुत लोग ग़लत लिखते/पढ़ते हैं,
अल्लह रे चश्म-ए-यार की मोजिज़-बयानियाँ
हर इक को है गुमाँ कि मुख़ातब हमीं रहे
इसके दूसरे मिसरे में बहुत से लोग मुख़ातिब पढ़ते हैं। शेर में बात हो रही है यार की आँखों के करिशमे की, कि वो आँखें जब बात करती हैं तो हर एक को लगता है कि उसी से बात हो रही है।
मुख़ातिब कहते हैं बात करने वाले को।
मुख़ातब उसे कहते हैं जिससे बात की जाये।
तो समझ में आया कि दूसरे मिसरे में सही तलफ़्फ़ुज़ मुख़ातब है। इसी लिये लिपि के साथ साथ ज़बान का इल्म भी होना चाहिये और मज़मून के सियाक़-ओ-सबाक़ (प्रसंग) से वाक़फ़ियत भी, उर्दू में ख़ासतौर से यह ज़रूरी हो जाता है। वरना कभी कभी ऐसी अजीब सूरत-ए-हाल से भी दो-चार होना पड़ सकता है जिसे मैंने इस शेर में बाँधा है,
“बढ़िया हो तुम” लिखा था मगर “बुढ़िया” पढ़ लिया
ज़ेर-ओ-ज़बर ने इश्क़ ही ज़ेर-ओ-ज़बर किया
हालाँकि वो इश्क़ ही क्या जो उम्र जैसी चीज़ को मेयार बनाये, मगर कनवेंशनल सूरत-ए-हाल में बदक़िसमती से यही सब होता है।
NEWSLETTER
Enter your email address to follow this blog and receive notification of new posts.




