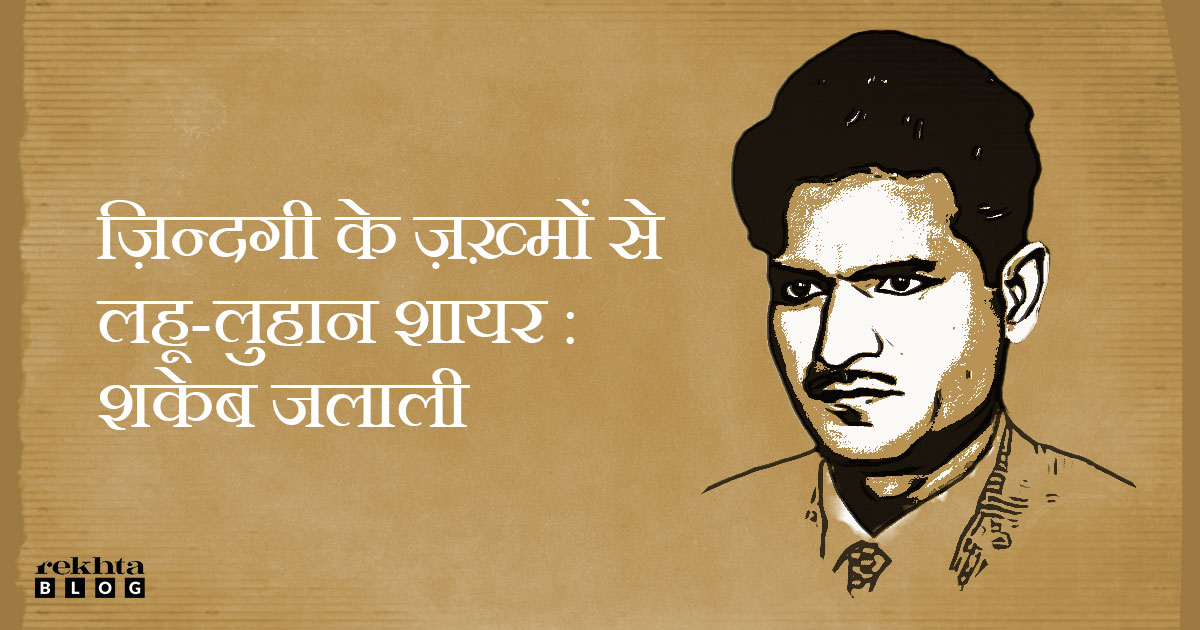
ज़िन्दगी के ज़ख़्मों से लहू-लुहान शायर : शकेब जलाली
आज शकेब जलाली साहब को ख़ुद-कुशी का रास्ता इख़्तियार किए 54 बरस गुज़र गए। ये बात ज़हन में आते ही कई ख़यालात और सवाल एक साथ आते हैं। पहले तो अल्बेयर कामू की तहरीर The Myth of Sisyphus से एक मामूली नज़र आने वाली सत्र : “There is but one truly serious philosophical problem and that is suicide.” फिर ये सवाल कि वो क्या असबाब हो सकते हैं जिनके असर में कोई मौत का रास्ता अपने लिए मुंतख़ब करता है। और फिर ये शेर:
इक आह भरना ‘शकेब’ हमसे ख़िज़ाँ-नसीबों को याद करके
कलाइयों में जो टहनियों की महकती कलियों का हार देखो
जब उनकी उम्र 9 बरस की थी, उनके वालिद ने बरेली जं० रेलवे स्टेशन के नज़दीक ज़हनी तवाज़ुन खो कर अपनी बीवी को रेलगाड़ी के सामने हलाक होने के लिए फेंक दिया था। ग़ालिबन उन्होंने ये लहू-लुहान मंज़र अपनी आँखों से देखा होगा। ये हादसा किस तरह उनकी नफ़सियात पर असर-अंदाज़ हुआ, इसका अंदाज़ा कुछ इस बात से भी हो जाता है कि उन्होंने ख़ुद-कुशी का यही तरीक़ा बाद में अपने लिए मुंतख़ब किया। ये हादिसा वो लहू-लुहान परिंदा बन कर गिरा, जिसका निशान किसी चटान पर भी सब्त हो जाता।
आ कर गिरा था कोई परिंदा लहू में तर
तस्वीर अपनी छोड़ गया है चटान पर
इस हादसे का लहू रिसता हुआ उनकी शायरी तक भी पहुँचा।
फ़सील-ए-जिस्म पे ताज़ा लहू के छींटे हैं
हुदूद-ए-वक़्त से आगे निकल गया है कोई
मौज-ए-सबा रवाँ हुई, रक़्स-ए-जुनूँ भी चाहिए
ख़ेमा-ए-गुल के पास ही दजला-ए-ख़ूँ भी चाहिए
कहा जाता है उन्होंने शायरी का आग़ाज़ 1947 में किया, जब उनकी उम्र 13 बरस की थी। उनकी शाइरी में मुझे एक मुसलसल सफ़र दिखाई देता है। उनकी शाइरी में हर तरह के मनाज़िर रू-नुमा होते हैं। अलग अलग पड़ाव आते हैं। राह में मुल्क-ए-सुख़न भी आता है और धूप-नगर भी।
ये काएनात है मेरी ही ख़ाक का ज़र्रा
मैं अपने दश्त से गुज़रा तो भेद पाए बहुत
जब ये शह-सवार अपने सफ़र का आग़ाज़ करता है तो तमाम ख़ुश-नुमा मंज़र नज़र आते हैं।
खिली है दिल में किसी के बदन की धूप ‘शकेब’
हर एक फूल सुनहरा दिखाई देता है
चूमा है मेरा नाम लब-ए-सुर्ख़ ने ‘शकेब’
या फूल रख दिया है किसी ने किताब में
वो उसका अक्स-ए-बदन था कि चाँदनी का कँवल
वो नीली झील थी या आसमाँ का टुकड़ा था
मुहावरा है कि कुआँ चल कर प्यासे के क़रीब नहीं आता। लेकिन वो इस तरह के करम को अपने ही अंदाज़ में ठुकरा देते हैं:
ख़ुद्दार हूँ क्यों आऊँ दर-ए-अहल-ए-करम पर
खेती कभी ख़ुद चल के घटा तक नहीं आती
इसी सिलसिले में उनका एक और शेर याद आता है:
दिल सा अनमोल रतन कौन ख़रीदेगा ‘शकेब’
जब बिकेगा तो ये बे-दाम ही बिक जाएगा
ये हैरत-कुन मनाज़िर उसे आमादा-ए-सफ़र रखते हैं:
इक याद है जो दामन-ए-दिल छोड़ती नहीं
इक बेल है जो लिपटी हुई है शजर के साथ
साया नहीं था नींद का आँखों में दूर तक
बिखरे थे रौशनी के नगीं आसमान पर
मगर ये सफ़र फ़क़त मसरूर-कुन मनाज़िर का मजमूआ’ भी तो नहीं। मनाज़िर बदलते हैं, मौसम पलटते हैं:
सितारे सिसकियाँ भरते थे, ओस रोती थी
फ़साना-ए-जिगर-ए-लख़्त-लख़्त ऐसा था
न इतनी तेज़ चलो सरफिरी हवा से कहो
शजर पे एक ही पत्ता दिखाई देता है
कमरे ख़ाली हो गए सायों से आँगन भर गया
डूबते सूरज की किरनें जब पड़ीं दालान पर
सफ़र से हैरत रफ़्ता-रफ़्ता ग़ायब होती जाती है और थकन ब-रू-ए-कार आती है:
ख़मोशी बोल उठ्ठे, हर नज़र पैग़ाम हो जाए
ये सन्नाटा अगर हद से बढ़े, पैग़ाम हो जाए
क्या जानिए कि इतनी उदासी थी रात क्यों
महताब अपनी क़ब्र का पत्थर लगा मुझे
कितनी गुम-सुम मिरे आँगन से सबा गुज़री है
इक शरर भी न उड़ा रूह की ख़ाकिस्तर से
लेकिन क्या ये सफ़र कभी ख़त्म हो सकता है?
उतर के नाव से भी कब सफ़र तमाम हुआ
ज़मीं पे पाँव धरा तो ज़मीन चलने लगी
उनकी शायरी का उस्लूब मुनफ़रिद और मुमताज़ है और उनकी ग़ज़ल में क़ुदरत, रात-दिन, जंगल-सेहरा, बहार-ख़िज़ाँ, अपने हर रूप में जलवा-नुमा है। उनकी शाइरी में ख़िज़ाँ-रसीदा शजर, चाँद, दरिया के इस्तिआरे क़सरत से इस्तेमाल हुए हैं। उनके लिए क़ुदरत के अज्ज़ा उनकी शाइरी में सिर्फ़ जमालियाती असासा बन कर नहीं रहते, बल्कि उनके रफ़ीक़ नज़र आते हैं। उन्होंने किस तरह चाँद को अपना शरीक-ए-सफ़र बना लिया है, इस शे’र में देखिए:
मैंने उसे शरीक-ए-सफ़र कर लिया ‘शकेब’
अपनी तरह से चाँद जो बे-घर लगा मुझे
यही चाँद ख़िज़ाँ-रसीदा होने के बा-वजूद झुक कर, रफ़ाक़त के बाइस शकेब से सवाल करता है:
ख़िज़ाँ के चाँद ने पूछा ये झुक के खिड़की में
कभी चराग़ भी जलता है इस हवेली में ?
ऐसा भी नहीं है कि शकेब की शाइरी शहरी मनाज़िर से आरी है, और बस क़ुदरत की ओट में सर-गरदाँ है। ये घाटियों और पर्बतों के मनाज़िर सिर्फ़ तख़य्युल के तख़्लीक़-कर्दा नहीं हैं। उनका का एक शेर है:
शब-ए-सफ़र थी, क़बा तीरगी की पहने हुए
कहीं कहीं पे कोई रौशनी का धब्बा था
जब इस शेर का लफ़्ज़-लफ़्ज़ तस्वीर बन के उभरता है, तो एक तरफ़ ये लगता है जैसे वक़्त के ला-मुतनाही सफ़र में दिन की जानिब सरगर्दां है और रात के दामन में कहीं कहीं एक सितारा टिमटिमा कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला देता है और दूसरी तरफ़ ये लगता है जैसे एक नीम-शब रेलगाड़ी चल रही है और कोई शख़्स खिड़की पर बैठा बाहर, कहीं दूर नज़र गड़ाए हुए है। शदीद तीरगी का आलम है और कभी कभी, कहीं दूर कोई जलता हुआ बल्ब, कोई रौशनी का कोई सुराग़ नज़र आ जाता है।
ब-क़ौल-ए-अहमद नदीम क़ासमी शकेब अपने आख़िरी दिनों में अक्सर ये कहा करते थे कि “मुझे ख़त आते हैं जिनमें मुझ से यही कहा जाता है कि तुम्हारी क़ुर्बानी देने का वक़्त आ गया है।” इस क़ुर्बानी के क्या मा’नी हो सकते हैं? शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी साहब ने शकेब के हवाले से लिखते हुए अमीर ख़ुसरो का एक क़ौल पेश-ए-नज़र रखा है : “फ़न-ए-शेर में उस्ताद बनने या उस्ताद कहलाने के लिए शर्तों का पूरा होना ज़रूरी है। एक शर्त ये है कि शायर का अदबी मुआशरा उसको उस्ताद माने।” ये बात सच है कि शकेब अपने फ़न में उस बुलंदी पर फ़ाएज़ थे जिस पर उन्हें तस्लीम न करना किसी अदबी हलक़े के लिए मुमकिन ही नहीं था। लेकिन शकेब को फिर भी वो तवज्जोह नहीं दी जा सकी जिसके वो मुस्तहक़ थे। उनकी किताब ‘रौशनी ऐ रौशनी’ अहमद नदीम क़ासमी के मक्तबा-ए-फ़ुनून और मावरा पब्लिशर्स से शाया’ हुई। कई कई एडिशन शाया’ हुए। लेकिन कोई तो सबब होगा कि ये मजमूआ’ पहली दफ़’अ उनके इंतिक़ाल के 6 बरस बाद शाया’ हुआ। वो यक़ीनन पूरे अदबी मंज़र-नामे से ना-ख़ुश थे। उनका एक शेर है:
थे हादसों के वार तो कारी, मगर मुझे
मरने नहीं दिया ख़लिश-ए-इंतिक़ाम ने
जब बे-कसी एक हद से गुज़रने लगती है तो इंसान इस ला-चारी से इख़्तिलाफ़ करते हुए अपनी बे-बसी को भी बग़ावत की अलामत बना लेता है। इंतिक़ाम की इकलौती सूरत इंतिक़ाम रह जाती है, फिर वो मुख़ालिफ़ से लिया जाए, या ख़ुद से। इंसान किसी ज़र्द सूरज की तरह रफ़्ता रफ़्ता डूबता चला जाता है।
झुकी चटान, फिसलती गिरफ़्त, झूलता जिस्म
मैं अब गिरा ही गिरा तंग-ओ-तार घाटी में
तूने कहा न था कि मैं कश्ती पे बोझ हूँ
आँखों को अब न ढाँप मुझे डूबते भी देख
उसका डूबना किसी पे ज़ाहिर नहीं होता, जब तक कि वो इस दर्जा न डूब जाए कि साँस भी साथ छोड़ दे।
इक साँस की तनाब जो टूटी तो ऐ ‘शकेब’
दौड़े हैं लोग जिस्म के ख़ेमे को थामने
लोग जब कुछ समझते हैं और उसे आवाज़ देते हैं, तब तक मुसाफ़िर तेज़ क़दमों से आख़िरी मंज़िल से भी आगे गुज़र चुका होता है और तमाम हुदूद-ए-वक़्त तोड़ कर बहुत दूर निकल चुका होता है। बा-वजूद इसके कि हस्ती की शमअ’ बुझ जाए, कुछ सुलगता हुआ रह जाता है।
मिशअल-ए-दर्द जो रौशन देखी
ख़ाना-ए-दिल को मुनव्वर जाना
यही माँद सी लौ, ये मिशअल-ए-दर्द आज भी रौशन है, और हमेशा रौशन रहेगी।
NEWSLETTER
Enter your email address to follow this blog and receive notification of new posts.




