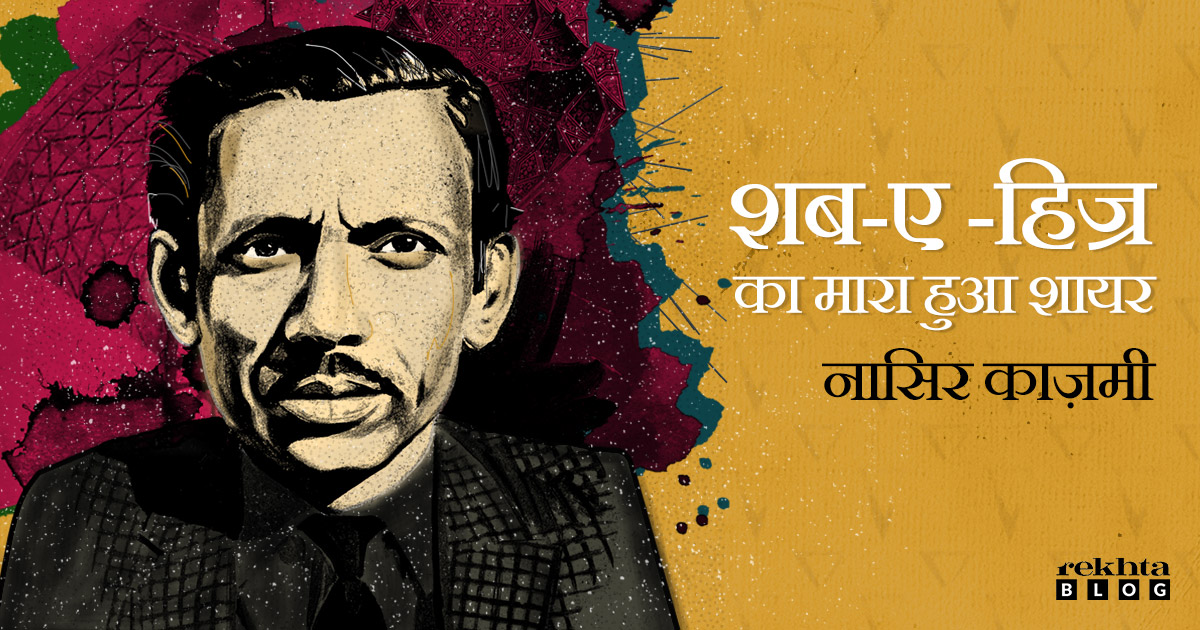
नासिर काज़मी ज़िन्दगी भर अपनी धरती अंबाला को याद करते रहे
उजले-उजले से कफ़न में सहर-ए-हिज्र ‘फ़िराक़’
एक तस्वीर हूँ मैं रात के कट जाने की
नासिर काज़मी पर फ़िराक़ साहब के एक शेर से बात करना शायद अजीब हो, लेकिन बे-सबब बिलकुल नहीं है। इसके चंद असबाब हैं। अव्वल तो ये कि फ़िराक़ उन शायरों में थे, जिन्होंने नासिर को सबसे ज़्यादा मुतअस्सिर किया। फ़िराक़ क़ाफ़िला-ए-ग़ज़ल को उस मोड़ तक ले आए थे जहाँ से उर्दू ग़ज़ल नासिर के तर्ज़-ए-बयान की तरफ़ रुख़ कर पाती। नासिर की शायरी मुख़्तलिफ़ मौज़ूआत पर फैली हुई है और इंसानी दर्द के तमाम अश्काल उनकी शायरी में नज़र आ जाते हैं – हिज्र से हिजरत तक। लेकिन जब इन तमाम मौज़ूआत को मजमूई तौर पर देखा जाए तो ग़ालिबन जो तस्वीर बनेगी, वो रात के कट जाने की होगी। नासिर ही के अशआर हैं:
ये ठिठुरी हुई लम्बी रातें कुछ पूछती हैं
ये ख़ामुशी-ए-आवाज़-नुमा कुछ कहती है
सब अपने घरों में लम्बी तान के सोते हैं
और दूर कहीं कोयल की सदा कुछ कहती है

नासिर के यहाँ रात बेहद वसीअ है। रात के मुख़्तलिफ़ पहलू उनकी शायरी में मौजूद हैं। कहा जाता है कि वो सारी सारी रात जागते रहते, और जब पौ फटती, परिंदे चहचहाना शुरू करते तब जा कर उनकी आँखों में नींद का कोई निशान नज़र आता। रात के मौज़ू पर कहे गए अशआर की उनके कुल्लियात में भरमार है:
कहाँ है तू कि तिरे इंतिज़ार में ऐ दोस्त
तमाम रात सुलगते हैं दिल के वीराने
मैं सोते सोते कई बार चौंक चौंक पड़ा
तमाम रात तिरे पहलुओं से आँच आई
तुझ को हर फूल में उर्यां सोते
चाँदनी-रात ने देखा होगा
रात कितनी गुज़र गई लेकिन
इतनी हिम्मत नहीं कि घर जाएँ
वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का
जो पिछली रात से याद आ रहा है

उनका पहला शेरी मजमूआ ‘बर्ग-ए-नय’ नाम से 1952 में शाया हुआ, जिसने मौजूदा शायरी के लिए एक नया मेयार तय कर दिया। दूसरा मजमूआ ‘दीवान’ नाम से 1972 में शाया हुआ। इसी तसलसुल में ‘पहली बारिश’ का ज़िक्र कर देना भी लाज़िम है। पहली बारिश अपनी ही तरह का एक मजमूआ’-ए-कलाम है जो 22 ग़ज़लों पर मुश्तमिल है। ये ग़ज़लें उन्होंने बांग्लादेश घूमने के बाद लिखी थीं। इन ग़ज़लों की एक ख़ूबी तो ये है कि इसकी तमाम ग़ज़लें एक ही ज़मीन पर हैं। यानी एक ही रदीफ़, क़ाफ़िया और बह्र। सारी ग़ज़लें ‘मुसलसल’ ग़ज़लें हैं। लेकिन इससे भी ज़ियादा दिलचस्प बात ये है कि ये सारी ग़ज़लें आपस में भी एक दूसरे से रब्त रखती हैं और एक मुसलसल सफ़र की तस्वीर पेश करती हैं। इन ग़ज़लों में एक इंसान की दास्तान मिलती है, जो मुहब्बत करता है। मजमूआ’ इस ग़ज़ल से शुरू होता है:
मैं ने जब लिखना सीखा था
पहले तेरा नाम लिखा था
मैं वो सब्रे-समीम हूँ जिस ने
बारे-अमानत सर पे लिया था
मैं वो इस्मे-अज़ीम हूँ जिस को
जिन्नो-मलक ने सज्दा किया था
पहली बारिश भेजने वाले
मैं तेरे दर्शन का प्यासा था
इस ग़ज़ल में इंसान की अज़मत पर खुल कर बात की गई है। इंसान के एक बेजा शय होने के तसव्वुर से शायर इंकार करते हुए कहता है कि वो वही है जिसे तमाम जिन्न-ओ-मलक ने सजदा किया था। आगे की ग़ज़लों में शायर अपने तअल्लुक़ के हवाले से बात करते है।
तू जब मेरे घर आया था
मैं इक सपना देख रहा था
चाँद की धीमी धीमी ज़ौ में
साँवला मुखड़ा लौ देता था
इन ग़ज़लों में फ़ितरत और ज़बान की ख़ूबसूरती अपने उरूज पर देखी जा सकती है। ऐसे शेर क़सरत से दस्तयाब होते हैं जिनकी मिसाल और किसी की शायरी में ढूँढ पाना मुश्किल है। मसलन:
शाम का शीशा काँप रहा था
पेड़ों पर सोना बिखरा था
दीवारों से आँच आती थी
मटकों में पानी जलता था
तेरे आँगन के पिछवाड़े
सब्ज़ दरख़्तों का रमना था
लाल खजूरों की छतरी पर
सब्ज़ कबूतर बोल रहा था
इक पाँव में फूल सी जूती
इक पाँव सारा नंगा था
जगमग-जगमग कंकरियों का
दश्ते-फ़लक में जाल बिछा था
सूरज, चाँद, पेड़, धूप, साये जीते-जागते से मालूम होते हैं। मसलन:
दिन का फूल अभी जागा था
धूप का हाथ बढ़ा आता था
तेरे घर के दरवाज़े पर
सूरज नंगे पाँव खड़ा था
दूर के पेड़ का जलता साया
हम दोनों को देख रहा था
धूप के लाल हरे होंटों ने
तेरे बालों को चूमा था

लेकिन धीरे धीरे ये तअल्लुक़ बिखरने की सम्त माइल हो जाता है और शायर आख़िर में फिर से तन्हाई की ओट में चला जाता है। नरगिस का फूल अना की अलामत समझा जाता है, तअल्लुक़ अना की नज़्र होने लगा है, इसका बयान देखिए:
काले पत्थर की सीढ़ी पर
नर्गिस का इक फूल खिला था
ये बात आगे चल कर और वाज़ेह होती है और आख़िर में शायर कह ही देता है:
अब मैं समझा, अब याद आया
तो उस दिन क्यों चुप-चुप सा था
दिल को यूँही सा रंज है वर्ना
तेरा मेरा साथ ही क्या था
तन्हाई मिरे दिल की जन्नत
मैं तन्हा हूँ, मैं तन्हा था
किस-किस बात को रोऊँ ‘नासिर’
अपना लहना ही इतना था
बासिर सुल्तान काज़मी, जो कि नासिर काज़मी साहब के बेटे हैं, ने इन ग़ज़लों के हवाले से लिक्खा है : ‘पहली बारिश’ के शायर की कहानी ये बताती है कि इंसान इस दुनिया में न सिर्फ़ अकेला आता है और यहाँ से अकेला जाता है, बल्कि वो यहाँ रहता भी अकेला ही है।

शेरी मजमूओं के सिवा उनका एक ड्रामा ‘सुर की छाया’ नाम से शाया हुआ, और निशात-ए-ख़्वाब नाम से नज़्मों का एक मजमूआ भी मंज़र-ए-आम पर आया।
नासिर की शायरी हिजरत के दर्द का एक अहम दस्तावेज़ भी है। नासिर अंबाला के थे और हिन्दोस्तान की तकसीम के बाद वो पाकिस्तान चले गए लेकिन अपनी ज़मीन से जुड़े होने के बावजूद उससे बिछड़ जाने का दर्द उनकी ज़िंदगी और शायरी का एक हिस्सा बन गया। क़सीदे की शक्ल में लिखी गई उनकी नज़्म, निशात-ए-ख़्वाब में उन्होंने अंबाला को याद किया है।
अंबाला एक शहर था सुनते हैं अब भी है
मैं हूँ उसी लुटे हुए क़र्ये की रौशनी
ऐ साकिनान-ए-ख़ित्ता-ए-लाहौर देखना
लाया हूँ उस ख़राबे से मैं लाल-ए-मादनी
ख़ुश रहने के हज़ार बहाने हैं दहर में
मेरे ख़मीर में है मगर ग़म की चाशनी
ये दर्द कभी शदीद टीस बन कर नज़र आता है तो कभी एक नग़्मा सा बन कर सुनाई पड़ता है, लेकिन ये दर्द एक सदा-ए-मुसलसल बन कर मौजूद रहता है। ये ग़म की चाशनी उदासी की भी मुख़्तलिफ़ अश्काल को सामने लाती है। मसलन:
हमारे घर की दीवारों पे ‘नासिर’
उदासी बाल खोले सो रही है
चहकते बोलते शहरों को क्या हुआ ‘नासिर’
कि दिन को भी मिरे घर में वही उदासी है
तन्हाई ब-ख़ुद एक अज़ाब है लेकिन अपनों को खोने के बाद की तन्हाई सर-ब-सर अज़ाब की इंतिहा मालूम होती है। उनकी हिजरत ने उन्हें इस तजर्बे से पूरी तरह मानूस कर दिया था।
ऐ सुकूत-ए-शाम-ए-ग़म ये क्या हुआ
क्या वो सब बीमार अच्छे हो गए
खोये हुए लोगों के बारे में वो कहते हैं:
मिल ही जाएगा रफ़्तगाँ का सुराग़
और कुछ दिन फिरो उदास उदास
मुश्किल है फिर मिलें कभी याराने-रफ़्तगाँ
तक़दीर ही से अब ये करामात हो तो हो
और रफ़्तगाँ के सुराग़ की तलाश में उदास उदास फिरते हुए, वो दुनिया से गुज़र जाते हैं। जाते जाते भी वो कहते हैं:
दाएम आबाद रहेगी दुनिया
हम न होंगे कोई हम सा होगा
यानी ये दुःख का सिलसिला जारी रहेगा, बस इसे भोगने वाले बदलते रहेंगे। यही शेर उनके कत्बे पर भी लिखा हुआ है।
NEWSLETTER
Enter your email address to follow this blog and receive notification of new posts.




